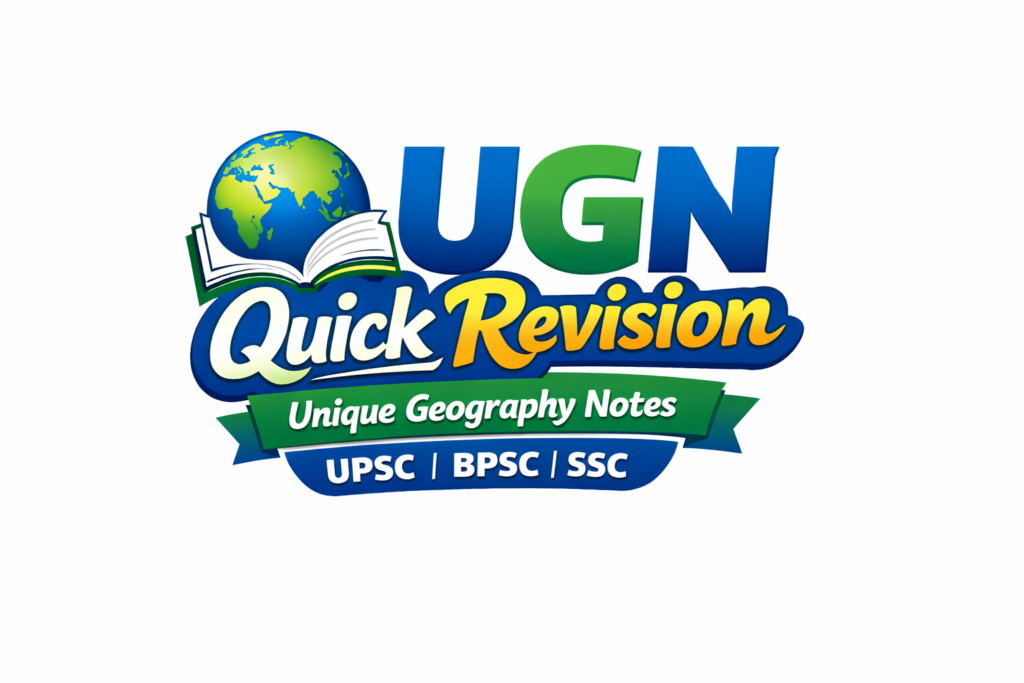3. Type of Rural Settlement (ग्रामीण बस्ती के प्रकार)
3. ग्रामीण बस्ती के प्रकार
(Type of Rural Settlement)

बस्ती (Settlement)
पृथ्वी के धरातल का वह स्थान जहाँ पर मानव सामूहिक रूप से अधिवास करता है, उस स्थान को बस्ती कहते हैं।
बस्ती दो प्रकार के होते हैं:-
(1) नगरीय बस्ती (Urban settlement) और
(2) ग्रामीण बस्ती (Rural settlement)
ग्रामीण बस्ती वह है जहाँ की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। जहाँ की जनसंख्या का आकार छोटी होती है तथा जनसंख्या में घनत्व कम होता है। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। वहीं भारत की लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं।
भौगोलिक कारक:-
ग्रामीण बस्तियों की उत्पत्ति एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक:
(A) प्राकृतिक कारक (Natural factors):
(i) जलवायु (Climate)
(ii) उच्चावच (Relief)
(iii) जल की उपलब्ध (Availability of water)
(iv) मिट्टियां (Soils)
(v) सूर्य प्रकाश (Sunlight)
(Vi) वनस्पति (Vegetation)
(B) आर्थिक एवं सामाजिक कारक (Economic and social factors):-
(i) आर्थिक व्यवसाय (Economic Business)
(ii) कृषि व्यवस्था (Agricultural system)
(iii) फसल प्रतिरूप (Cropping pattern)
(iv) परिवहन व्यवस्था (Transportation)
(v) सुरक्षा (Security)
(C) ऐतिहासिक एवं राजनितिक कारक (Historical and political factors):-
(i) जाति व्यवस्था (Caste system)
(ii) जनसंख्या (Population)
(iii) सामाजिक एवं रूढ़ियाँ (Social and conventions)।
ग्रामीण बस्तियों के प्रकार (Types of rural settlements)
ग्रामीण बस्तियों का प्रकार किसी बस्ती में मकानों की संख्या एवं मकानों के बीच की पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। मोटे तौर पर ग्रामीण बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, जो निम्नवत है :-
(1) गुच्छित ग्रामीण बस्ती/सघन ग्रामीण बस्ती (Compact Settlement)
(2) प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती/बिखरी बस्तियाँ (scattered settlements)
(1) गुच्छित ग्रामीण बस्ती/सघन ग्रामीण बस्ती (Compact Settlement)
अमेरिकी भूगोलवेत्ता प्रेसी ने गुच्छित ग्रामीण बस्ती को “Compact Anglomeration” से सम्बोधित किया है। वैसी ग्रामीण बस्ती जिसमें अधिवासीय मकान एक-दूसरे से बिल्कुल सटे-2 हो, वैसी ग्रामीण बस्ती को ही गुच्छित ग्रामीण बस्ती कहते हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्ती की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है –
(i) मकानों के बीच की दूरी बहुत कम होती है।
(ii) कम स्थान पर अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं।
(iii) सड़क एवं गलियाँ पूर्णरूपेण विकसित नहीं होती है।
(iv) ऐसी बस्तियाँ प्रायः (मानसूनी जलवायु क्षेत्रों) में पायी जाती है।
गुच्छित ग्रामीण बस्तियों के विकास के कारण
(Reasons for the development of clustered rural settlements)
गुच्छित ग्रामीण बस्तियों के विकास के पीछे निम्नलिखित कारण सक्रिय होते हैं-
(i) बाढ़ के मैदान में अधिवास करने योग्य भूमि का अभाव होता है। इसलिए उन क्षेत्रों में मिलने वाला प्राकृतिक बाँध तथा ऊँचे-2 स्थानों पर गुच्छित बस्तियाँ विकसित हो जाती है।
नोट:- सघन बस्ती (Compact Settlement) को संकेन्द्रित (Concentrated), पुंजित (Clustered), नाभिकीय (Nucleated) एवं एकत्रित/ गुच्छित (Agglomerated) बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है।
(ii) मरुस्थलीय क्षेत्रों में गुच्छित बस्तियों का विकास होता है क्योंकि सभी घर के लोग जल स्रोतों से जुड़े हुए रहना चाहते हैं।
(iii) पर्वतीय कटकों के सहारे भी गुच्छित बस्तियां विकसित होती है। जैसे- नागा जनजाति के लोग जानवरों एवं कुकी जनजातियों की भय से पहाड़ों की चोटियों पर निवास करते हैं। चोटियों पर कम भूमि उपलब्ध होने के कारण बस्तियाँ गुच्छित हो जाती है।
(iv) बाढ़ के मैदान में उपजाऊ एवं उर्वर भूमि का महत्त्व अधिक होता है। किसान चप्पे-2 भूमि का प्रयोग कर उसका सदुपयोग करना चाहता है, जिसके कारण अधिवास जैसे अनुत्पादक कार्य के लिए भूमि कम बच जाती है। फलतः गुच्छित बस्तियों का विकास हो जाता है।
(v) मानसूनी प्रदेशों में और बाढ़ वाले क्षेत्रों में श्रम प्रधान चावल की खेती की जाती है। अत: श्रम की पूर्ति बनाये रखने के लिए गुच्छित ग्रामीण बस्तियों का विकास होता है।
(vi) एक सांस्कृतिक विशेषता रखने वाले लोगों के बीच विशेष भावनात्मक लगाव होता है। अतः एक ही धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति के लोग गुच्छित अधिवास करने की प्रवृति रखते हैं। आज भी भारत गाँवों में जातीय टोले मिलते हैं।
(vii) लुटेरों की भय, सामाजिक तनाव, जंगली जानवरों का आक्रमण इत्यादि कुछ ऐसे अन्य कारण है जो गुच्छित ग्रामीण बस्ती के विकास को प्रेरित करती हैं।
गुच्छित ग्रामीण बस्तियों के लाभ और हानियाँ
(Advantages and Disadvantages of Clustered Rural Settlements)
गुच्छित बस्तियों के कुछ लाभ और कुछ हानियाँ दोनों हैं। जैसे:-
गुच्छि बस्ती के लाभ (Benefits of cluster settlement)
(i) सामुदायिक भावना का विकास होता है।
(ii) लोग सुख-दुःख में एक-दूसरे के सहभागी बनते हैं।
(iii) श्रम आधारित सघन कृषि का विकास होता है।
गुच्छित बस्ती के हानि (Disadvantages of clustered settlement)
(i) गुच्छित बस्तियों में किसी भी व्यक्ति का जीवन निजी नहीं रह जाता है। जब निजी जीवन प्रभावित होता है तब संपूर्ण ग्रामीण बस्ती में अशान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है।
(ii) गुच्छित बस्तियों में अधिवासीय जमीन का अभाव होता है जिसके कारण भूमि की माँग बढ़ जाती है जिससे लोग दूसरे की जमीन हड़पने लगते हैं। फलतः ग्रामीण लोग कानूनी जटिलताओं में फँसकर अपना जीवन व्यर्थ गवाँ देते हैं।
नोट :- गुच्छित = पूँजित = सघन
(iii) गुच्छित बस्तियाँ आलसी लोगों की बस्तियाँ कहलाती है। आलस्यपन का कारण मकानों का नजदीक होना है। इससे लोगों के कार्मिक क्षमता में कमी आती है।
गुच्छित ग्रामीण बस्ती के प्रकार (Types of clustered rural settlement)
गुच्छित बस्तियाँ पाँच प्रकार के होती हैं-
(a) मानसूनी गुच्छित बस्ती (Monsoon clustered settlement):-
यह मानसूनी जलवायु प्रदेश में बाढ़ के मैदानों में दिखाई देती है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, निचली गंगा का मैदान, संपूर्ण बांग्लादेश, पूर्वी चीन के मैदान, ईरावदी का मैदान, मेकांग का मैदान, नील नदी के डेल्टा पर गुच्छित बस्तियाँ दिखाई देती हैं।
(b) लगभग गुच्छित बस्ती (Almost clustered settlements):-
ऐसी बस्तियाँ वैसे मानसूनी क्षेत्रों से विकसित होती है जहाँ पर बाढ़ की समस्या नहीं है। ये वैसी बस्तियाँ है जहाँ एक से अधिक गुच्छित बस्ती एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विकसित होते हैं। ऐसे बस्तियों में यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन बस्ती पुराना है और कौन बस्ती नवीन है तथा किस बस्ती के प्रति आकर्षण सर्वाधिक है?
ऐसी बस्ती उत्तर-पश्चिम भारत, सिन्धु के मैदान, उत्तरी चीन & नील नदी के ऊपरी भाग में ये बस्तियाँ मिलती हैं।
(c) रेखीय गुच्छित बस्ती (Linear clustered settlement):-
रेखीय गुच्छित बस्तियों का विकास राजमार्गो, नहरों, प्राकृतिक बाँधों के ऊपर होता है क्योंकि ग्रामीण बस्ती के प्रत्येक लोग राजमार्गों और नहरों की सुविधा समान रूप से लेना चाहते हैं। इन्दिरा गांधी नहर, सरहिन्द नहर, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र और उत्तरी चीन में नहरों के ऊपर विकसित गुच्छित बस्तियाँ मिलती हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक बाँध के ऊपर विकसित गुच्छित बस्तियाँ मिलती हैं जबकि भारत के तटीय मैदानी क्षेत्रों में राजमार्गो के किनारे गुच्छित बस्तियाँ मिलती हैं।
(d) गुच्छित सह पुरवा बस्ती (Clustered cum hamlet settlement):-
वैसी बस्ती जिसमें एक केन्द्रीय बस्ती सर्वाधिक अनुकूलन वाले स्थान पर विकसित होती है और उसके ईर्द-गिर्द छोटी बस्तियों का विकास हो जाता है। छोटी बस्ती को ही पुरवा बस्ती कहते हैं। छोटी बस्तियाँ और केन्द्रीय बस्ती एक-दूसरे से सांस्कृतिक कार्यों के लिए जुड़े हुए होते हैं। मानसूनी भारत में पुरवा बस्ती श्रमिकों की बस्ती होती है।
नोट- पुरवा = छोटी बस्ती या श्रमिकों की बस्ती
(e) गुच्छित सह पुरवा सह बिखरी बस्ती (Clustered cum hamlet cum scattered settlement):-
ऐसी बस्तियाँ मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में दिखाई देती है। पहला शोषण मूलक कृषि अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में, जैसे – बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश, इत्यादि में। दूसरा वैसे क्षेत्रों में जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूलित वातावरण सर्वत्र रूप से मौजूद है।
(2) प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती/बिखरी बस्तियाँ (Scattered rural settlement/scattered settlements)
प्रकीर्ण बस्ती को बिखरी हुई बस्ती भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिवासीय मकान एक-दूसरे से दूर-2 बने होते हैं।
प्रकीर्ण बस्तियों के विकास के कारण (Reasons for the development of scattered settlements)
प्रकीर्ण बस्तियों के विकास के निम्नलिखित कारण हैं।
(i) अधिवास की सुविधा सर्वत्र एक समान मौजूद होना। जैसे:- प० यूरोप
(ii) पर्याप्त समतल भूमि उपलब्ध न होना।
(iii) समाज में किसी भी प्रकार का भय, आतंक या तनाव का अभाव होना।
(iv) कभी-2 गाँवों में कुछ विशेष लोगों को रहने की इजाजद न किया जाना।
(v) नवीन आर्थिक गतिविधियों का विकास होना।
प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों के लाभ और हानियाँ (Advantages and Disadvantages of Scattered Rural Settlements)
प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों के लाभ (Advantages of scattered rural settlements)-
प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों के निम्नलिखित लाभ है-
(i) प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन सुरक्षित रहता है।
(ii) आर्थिक क्षमता अधिक होने के कारण ऐसे बस्ती के लोग अधिक सम्पन्न होते हैं।
प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों के हानि (Disadvantages of scattered rural settlements)-
प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियों का कुछ नाकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे –
⇒ लोग एकाकी जीवन जीते-2 एकाकी हो जाते हैं।
⇒ लोग एक-दूसरे के सुख-दु:ख में सहभागी नहीं बन पाते हैं।
⇒ आकस्मिक संकट आ जाने पर लोगों की स्थिति दयनीय हो जाती है।
⇒ लोगों को सभी प्रकार के कार्य स्वयं करने पड़ते हैं।
प्रकीर्ण बस्तियों के प्रकार (Types of Scattered settlements)
प्रकीर्ण बस्तियाँ भी पाँच प्रकार के होती हैं-
(i) एकाकी प्रकीर्ण बस्ती (Isolated scattered settlement):-
इसमें एक स्थान पर एक ही मकान स्थित होता है। यह विकसित देशों के गाँवों की विशेषता है। न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, USA, यूरोप में ऐसी बस्तियाँ मिलती हैं। उतर-पश्चिम भारत में भी ऐसी बस्ती विकास की प्रक्रिया से गुजर रही है।
(ii) बिखरी प्रकीर्ण बस्ती (Dispersed scattered settlement):- इसमें एक स्थान पर एक से अधिक मकान होते हैं लेकिन एक-दूसरे से काफी दूर होते हैं। पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार के बस्तियों का उदाहरण मिलता है। उ०-पूर्वी भारत के जनजातीय बस्तियाँ, मध्य अफ्रीका, मोजाम्बिक, आमेजन प्रदेश, केरल के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान के द०-पूर्वी पठारी क्षेत्रों में बिखरी प्रकीर्ण बस्तियाँ दिखाई देती है।
(iii) पुरवा प्रकीर्ण बस्ती (Purva scattered settlement):-
वैसे प्रकीर्ण बस्ती जिसमें कई मकान एक स्थान पर होते हैं लेकिन मकानों के बीच की दूरी अधिक होती है। इसमें बस्ती का कुल आकार छोटा होता है। ऐसी बस्तियों का विकास पठारी क्षेत्रों में प्रकीर्ण वस्ती वहाँ पर होता है जहाँ पर पेयजल और कृषि की संभनाएँ मौजूद है। ढक्कन का पठार, मेघालय के पठार पर ऐसी बस्ती मिलती है।
(iv) रेखीय प्रकीर्ण बस्ती (Linear scattered Settlement):-
रेखीय प्रकीर्ण बस्ती में अधिवासीय मकान एक ही रेखा में दूर-2 पर अवस्थित होते हैं। ऐसी बस्ती प्राकृतिक बांध, राजमार्ग, नहर, वनीय सड़क के किनारे पायी जाती है। इसका उदा० उन सभी क्षेत्रों में दिखाई देता है जहाँ पर उपरोक्त भौगोलिक कारक मौजूद है।
(v) सीढ़ीनुमा प्रकीर्ण बस्ती (Terraced Scattered Settlement):-
ऐसी बस्तियाँ पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा स्थलाकृति के सहारे विकसित होती है। अरुणाचल प्रदेश या हिमालय के ढालों पर, आल्पस एवं किलीमंजारो पर्वत के ढालों पर इस तरह के अनेक बस्तियाँ मिलती है।
निष्कर्ष-
इस तरह ऊपर के तथ्यों से स्पष्ट है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पूर्णत: भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है।
प्रश्न प्रारूप
Q. ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भारत के संदर्भ में उन बस्तियों की विशेषता और वितरण प्रारूप की चर्चा करें।
Q. ग्रामीण बस्तियाँ नगरीय बस्तियों से किस प्रकार भिन्न है? ग्रामीण बस्तियों के प्रकार तथा प्रतिरूप की विशेषता भारत के सन्दर्भ में विशेष रूप से करें।