20. Meaning and Scope of Economic Geography (आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय-क्षेत्र)
Meaning and Scope of Economic Geography
(आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय-क्षेत्र)
प्रश्न प्रारूप
Q. आर्थिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके विषय-क्षेत्र एवं नूतन प्रवृतियों की विवेचना कीजिए।
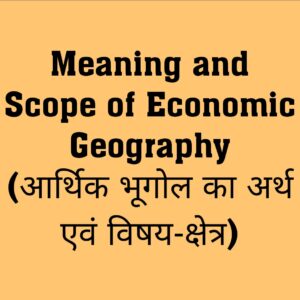
उत्तर- पृथ्वी मानव का घर है और मानव व पृथ्वी तल दोनों ही तथ्य अस्थिर एवं परिवर्तनशील हैं। पृथ्वी की भौतिक परिस्थितियों और मानव के कार्य-कलापों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन मानव भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के जन्मदाता गोट्ज (1882) थे। इसके अध्ययन में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन करते हैं। मानव की आकांक्षाएं एवं आवश्यकताएं अत्यधिक असीमित और विविध हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव अनेक वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता उनका क्रय करता है तथा अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं से उनका विनिमय करता है।
प्रो. मेकफरलेन के अनुसार आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम मानव के आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं।
प्रो. जी. चिशौल्म के अनुसार आर्थिक भूगोल में हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करती हैं।
इस अध्ययन के माध्यम से किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र के भावी आर्थिक और व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों के अध्ययन का सम्मिलित प्रभाव भी जाना जाता है।
सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हंटिंगटन जीविकोपार्जन प्रदान करने वाले सभी प्रकार के पदार्थों, साधनों, क्रियाओं, रीति-रिवाजों तथा मानव शक्तियों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में मानते हैं।
प्रो. शॉ के अनुसार मानव की आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगो, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुरूप होती हैं।
इसी प्रकार डॉ. एन. जी. जे. पाउण्ड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भू-पृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन है।
प्रो. रैयन तथा बैगस्टन के शब्दों में आर्थिक भूगोल के अध्ययन में विश्व के भिन्न-भिन्न भागों में मिलने वाले आधारभूत संसाधन एवं स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। इन स्रोतों के शोषण पर पड़ने वाली भौतिक परिस्थितियों के प्रभाव की विवेचना की जाती है। विभिन्न प्रदेशों के आर्थिक विकास के अन्तर की व्याख्या की जाती है।
भूगोल की अन्य शाखाओं की भांति आर्थिक भूगोल की विषय-वस्तु एवं विषय-क्षेत्र पर भूगोलवेत्ताओं के विचारों में पर्याप्त मतभेद रहा है। कुछ विद्वान मानव के भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के अध्ययन को अधिक महत्व देते हैं, तो कुछ मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा जीविकोपार्जन के अनेकानेक साधनों के अध्ययन को मुख्य मानते हैं। संक्षेप में विश्व के विभिन्न भागों में मिलने वाले खनिज, कृषि, औद्योगिक साधनों का उत्पादन, उपभोग, वितरण, परिवहन तथा व्यापारिक अध्ययन आर्थिक भूगोल के अन्तर्गत किया जाता है।
वर्तमान में मानव ने विज्ञान और तकनीक की सहायता से आशानुरूप विकास कर लिया है। मानव ने अपने आर्थिक क्षेत्र का विस्तार, समुद्र, भू-गर्भ और अन्तरिक्ष तक कर लिया है। व्यावहारिक जगत में आर्थिक भूगोल के अध्ययन का अत्यधिक महत्व है; इसके अध्ययन के माध्यम से कृषक, श्रमिक, व्यापारी, उद्योगपति तथा राजनीतिज्ञ सव ही लाभान्वित होते हैं।
विभिन्न देशों को अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने तथा विकास की भावी योजनाओं के निर्माण में आर्थिक भूगोल के अध्ययन को आधार बनाना पड़ता है। किसी प्रदेश के आर्थिक साधनों का उच्चतम सीमा तक विकास कर वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए जीविकोपार्जन के साधन सुलभ किए जा सकते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को सन्तुलित तथा मानव शक्ति को उत्पादन क्रिया से सम्बद्ध करने में आर्थिक भूगोल का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
मानव की आधुनिक अनुसन्धान एवं अन्वेषण की प्रवृत्ति ने मानव के आर्थिक क्रिया-कलापों को और अधिक विस्तृत बना दिया है।
इस विषय की मुख्य संकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) आर्थिक भू-दृश्य:-
इसमें किसी प्रदेश के आर्थिक व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया जाता है। मानव द्वारा प्राकृतिक साधनों के अधिकाधिक उपयोग पर बल दिया जाता है।
(2) गत्यात्मक आर्थिक भू-दृश्य:-
इस संकल्पना में सदैव परिवर्तन एवं विकास के तत्व को महत्व दिया गया है। जहां आर्थिक भू-दृश्य भूतकाल के आर्थिक कार्यों का परिणाम है, वहां गत्यात्मक आर्थिक भू-दृश्य पुरोगामी और भावी विकास की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है।
(3) वर्तमान आर्थिक भू-दृश्य:-
ये संसाधन, संरचना, आर्थिक विकास एवं आर्थिक प्रक्रिया द्वारा उपलब्धि के परिचायक हैं। वहां की आर्थिक स्थिति को विकासावस्था स्तर भी प्रकट करते हैं। युवावस्था में संसाधनों के शोषण के अवसर उपलब्ध रहते हैं; चरमोत्कर्ष की परिपक्व अवस्था में संसाधनो के उच्चतम उपभोग एवं वृद्धावस्था में विकास की अवरुद्ध एवं धीमी प्रगति के आसार दृष्टिगोचर होते रहते हैं।
(4) आर्थिक क्रिया-कलापों की स्थिति में सिद्धान्तों और नियमों के आधार पर स्थिति-स्थापना तथा वितरण की व्याख्या की जाती है। इसमे विषय-वस्तु उपागम तथा प्रादेशिक उपागम को आधार बना कर अध्ययन किया जाता है।
(5) क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं जैविक भिन्नता के अन्तर के परिणामस्वरूप उपलब्धि के स्तर में भी भिन्नता मिलती है।
(6) क्षेत्रीय क्रियात्मक अन्योन्यक्रिया में विभिन्न प्रदेशो में विचित्र-सा पारस्परिक क्रियात्मक अन्तर सम्बन्ध दृष्टिगोचर होता है। यह सम्बन्ध लम्बवत् और क्षैतिज दोनों प्रकार का होता है।
(7) भू-दृश्यों का क्षेत्रीय कार्यात्मक सगठन संकेन्द्रीय और समान दोनों प्रकार का होता है। इसमें पारस्परिक सम्बन्ध कहीं स्पष्ट तो कहीं अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट सम्बन्धों को परिवहन और संचारवाहन से सम्बद्ध किया जाता है।
(8) क्षेत्रीय आर्थिक विकास संकल्पना में विकास की तुलना, अन्य प्रदेशों से सांस्कृतिक तथा तकनीकी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर की जाती है। प्रगति के लिए क्षेत्र विशेष के आर्थिक संसाधनों के विकास पर अधिकाधिक बल दिया जाता है।
आर्थिक भूगोल के अध्ययन उपागम एवं विधियाँ
(APPROACHES AND METHODS OF ECONOMIC GEOGRAPHY)
आर्थिक भूगोल के सन्तुलित अध्ययन के लिए कई उपागमों व अध्ययन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक-दूसरे की पूरक हैं। निम्नांकित चार उपागम अध्ययन दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
(1) वस्तुगत उपागम (Commodity Approach):-
इस उपागम के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं, जैसे- गेहूं, चावल, गन्ना, लोहा, पेट्रोलियम आदि के उत्पादन एवं वितरण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। किन्तु कुछ विद्वान इस उपागम में वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण का विश्लेषण न करके व्यवसाय का वितरण और विश्लेषण करते हैं। जैसे- कृषि व्यवसाय, वस्तु संग्रह एवं आखेट व्यवसाय, खनन व्यवसाय, उद्योग आदि। इस कारण इस उपागम को ‘व्यवसाय उपागम’ (Occupational Approach) भी कहा जाता है।
(2) प्रादेशिक उपागम (Regional Approach):-
इस उपागम के अन्तर्गत सर्वप्रथम विश्व को कुछ बृहत् प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर लिया जाता है और प्रत्येक प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण तथा विभिन्न वस्तुओं के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है।
(3) सैद्धान्तिक उपागम (Theoretical Approach):-
इस उपागम के अन्तर्गत किसी भी वस्तु या प्रदेश की विशेषताओं एवं वितरण प्रतिरूप का अध्ययन पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों के सन्दर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन विधि से मुख्यतः सिद्धांतों को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है, न कि वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना।
(4) क्रमबद्ध उपागम (Systematic Approach):-
इस उपागम के अन्तर्गत वस्तुओं के वितरण की सामान्य विशेषताओं का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है। यह क्रमबद्ध अध्ययन तीन चरणों में सम्पन्न किया जाता है:-
(1) प्रथम चरण में किसी भी वस्तु की स्थिति तथा वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है।
(ii) द्वितीय चरण में उस वस्तु विशेष की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है।
(iii) तृतीय चरण में उस वस्तु का अन्य प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों से सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है। ये अन्तर्सम्बन्ध ‘कार्यकरण सम्बन्ध’ (Cause and Effect Relationship), ‘क्रियात्मक सम्बन्ध’ (Functional Relationship) तथा ‘क्षेत्रीय सम्बन्ध’ (Areal Relationship) के रूप व्यक्त किए जाते हैं।
