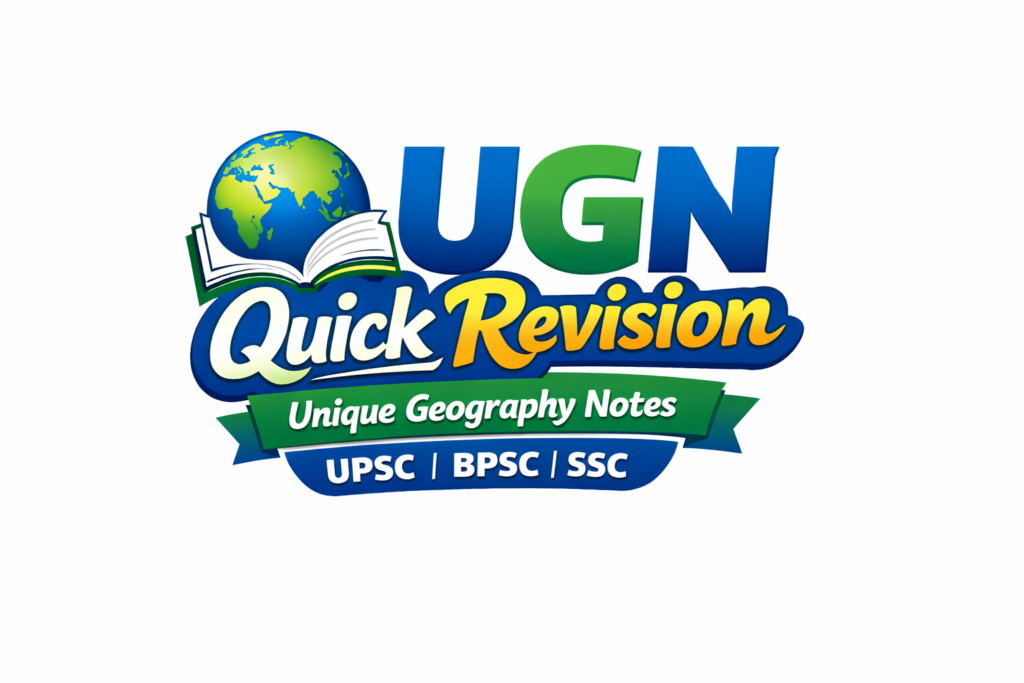44. Major tribal groups of India (भारत की प्रमुख जनजातीय समूह)
44. Major tribal groups of India
(भारत की प्रमुख जनजातीय समूह)
जनजातियाँ मुख्यतः वह मानव समुदाय हैं जो कि एक अलग निश्चित भू-भाग में निवास करती हैं और जिनकी एक अलग संस्कृति, रीति-रिवाज, भाषा होती है तथा ये केवल अपने ही समुदाय में विवाह करती हैं। सामान्य अर्थों में कहें तो जनजातियों का अपना एक वंशज, पूर्वज यहाँ तक कि देवी-देवता भी अलग होते हैं। ये प्राय: प्रकृति पूजक होते हैं।
भारत की जनजातियाँ देश के प्राय: सभी राज्यों में फैली हुई है। अलग-अलग राज्यों में इनके रीति-रिवाज और रहन सहन भी प्राय: अलग होते हैं। जनजातियाँ, भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के संविधान में इसके लिए अनुसूचित जनजाति (ST) शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं।
जनजाति, भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक शब्द भी है तो दूसरी ओर, इन्हें अन्य कई नामों से भी जानते है जैसे- आदिवासी, आदिम-जाति, वनवासी, प्रागैतिहासिक, असभ्य जाति, असाक्षर, निरक्षर तथा कबीलाई समूह इत्यादि।
मुख्य प्रजातीय विभाजन:
प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर, गुहा (1935) का मानना है कि वे निम्नलिखित तीन प्रजातियों से संबंधित हैं।
(i) मोगोलोइड्स
उत्तर एल्पाइन या मंगोलियन गोल सिर के होते हैं। इनके बाल सीधे और चपटे, चेहरा और जबड़ा नतोदर होता है। नाक पतली और संकरी, रंग हल्का पीला-सा खुमानी रंग का होता है। ये विशेषताएं भोटिया (मध्य हिमालय), वांचू (अरुणाचल प्रदेश), नागा (नागालैंड), खासी (मेघालय), आदि के बीच पाई जाती हैं।
(ii) प्रोटो ऑस्ट्रलॉयड्स
इस प्रजाति का सिर लम्बा और उभरा हुआ होता है। बाल पूर्णतः घुंघराले और त्वचा का रंग गहरे काले से लेकर कत्थई तथा हल्का पीला होता है। जबड़े कुछ निकले हुए और नाक साधारण रूप से चौड़ी होती है। ये विशेषताएं गोंड (मध्य प्रदेश), मुंडा (छोटानागपुर), हो (झारखंड) आदि में पाई जाती है।
(iii) नेग्रिटो
इस प्रजाति का रंग लाल चाकलेटी से लेकर काला कत्थई तक होता है। इनका डील-डौल नाटा (5 फुट से कम) होंठ काफी मोटे, नाक चौड़ी और चपटी होती है। इनके बाल चपटे, फीते के समान और घने होते हैं। वे आपस में लिपटकर गांठ का निर्माण करते हैं। इनमें जबड़े और दांत आगे निकले होते हैं। इस समय कुछ ही हजार नीग्रिटो जीवित हैं। उनमें अन्य जातियों के रक्त का मिश्रण हो गया है। ये विशेषताएं कादर (केरल), ओंगे (लिटिल अंडमान), जारवा (अंडमान द्वीप) आदि के बीच पाई जाती हैं।
जनजातियों का भौगोलिक वितरण
वर्तमान समय में भी भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनजातियों के साथ-साथ संस्कृति का विविधीकरण भी देखने को मिलता है। सम्पूर्ण भारत में जनजातियों की वास्तविक स्थिति उनके भौगोलिक वितरण को समझकर आसानी से लिया जा सकता है।
भौगोलिक आधार पर भारत की जनजातियों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। जैसे-
(i) उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र:-
उत्तर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत हिमालय के तराई क्षेत्र, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र सम्मिलित किये जाते हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बकरवाल, गुर्जर, थारू, बुक्सा, राजी, जौनसारी, शौका, भोटिया, गद्दी, किन्नौरी, गारो, खासी, जयंतिया इत्यादि जनजातियाँ निवास करती हैं।
(ii) मध्य क्षेत्र:-
मध्य क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के पठारी तथा पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि राज्य इस क्षेत्र में आते हैं जहाँ मुख्यतः भील, गोंड, रेड्डी, संथाल, हो, मुंडा, कोरवा, उरांव, कोल, बंजारा, मीणा, कोली आदि जनजातियाँ रहती हैं।
(iii) दक्षिण क्षेत्र:-
दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य आते हैं जहाँ मुख्य रूप से टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कडार, इरुला आदि जनजातियाँ बसी हुई हैं।
(iv) द्वीपीय क्षेत्र:-
द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान एवं निकोबार की जनजातियाँ आती हैं। जहाँ मुख्य रूप से सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन इत्यादि।
भारत की जनजातीय जनसँख्या
भारत में अनुसूचित जनजातियों (ST) की जनसँख्या 10.42 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। भारत में जनजातीय जनसंख्या अलग-अलग हिस्सों में फैली हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं।
भारत में अधिकतम जनजातीय जनसँख्या वाले पाँच राज्य है-
(i) मिजोरम (जनसंख्या का 94.4%)
(ii) लक्षद्वीप (94%)
(iii) नागालैंड (86.5%)
(iv) मेघालय (86.1%)
(v) अरुणाचल प्रदेश (68.79%)
इसके अलावा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में भी महत्वपूर्ण जनजातीय बस्तियाँ हैं।
भारत में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियाँ
भारत की सबसे अधिक ज्ञात जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, गारो, खासी, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडाबा और ग्रेट अंडमानी जनजातियाँ शामिल हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इन सभी जनजातियों में, भील आदिवासी समूह, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह देश की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का करीब 38% है।
नीचे राज्य और उनमें निवास करने वाले जनजातियों के समूहों के बारे में जानकारी दी जा रही है-
| राज्य | निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ |
| झारखण्ड | संथाल, असुर, बैगा, बन्जारा, बिरहोर, गोंड, हो, खरिया, खोंड, मुंडा, कोरवा, भूमिज, मल पहाडिय़ा, सोरिया पहाडिय़ा, बिझिया, चेरू लोहरा, उरांव, खरवार, कोल, भील। |
| बिहार | बैंगा, बंजारा, मुण्डा, भुइया, खोंड। |
| मध्य प्रदेश | भील, मिहाल, बिरहोर, गडावां, कमार, नट। |
| उड़ीसा | बैगा, बंजारा, बड़होर, चेंचू, गड़ाबा, गोंड, होस, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव, संथाल, सओरा, मुन्डुप्पतू। |
| मेघालय | खासी, जयन्तिया, गारो। |
| अरुणाचल प्रदेश | अबोर, अक्का, अपटामिस, बर्मास, डफला, गालोंग, गोम्बा, काम्पती, खोभा मिसमी, सिगंपो, सिरडुकपेन। |
| असम व नगालैंड | बोडो, डिमसा गारो, खासी, कुकी, मिजो, मिकिर, नगा, अबोर, डाफला, मिशमिस, अपतनिस, सिंधो, अंगामी। |
| तमिलनाडु | टोडा, कडार, इकला, कोटा, अडयान, अरनदान, कुट्टनायक, कोराग, कुरिचियान, मासेर, कुरुम्बा, कुरुमान, मुथुवान, पनियां, थुलया, मलयाली, इरावल्लन, कनिक्कर,मन्नान, उरासिल, विशावन, ईरुला। |
| कर्नाटक | गौडालू, हक्की, पिक्की, इरुगा, जेनु, कुरुव, मलाईकुड, भील, गोंड, टोडा, वर्ली, चेन्चू, कोया, अनार्दन, येरवा, होलेया, कोरमा। |
| आंध्र प्रदेश | चेन्चू, कोचा, गुड़ावा, जटापा, कोंडा डोरस, कोंडा कपूर, कोंडा रेड्डी, खोंड, सुगेलिस, लम्बाडिस, येलडिस, येरुकुलास, भील, गोंड, कोलम, प्रधान, बाल्मिक। |
| छत्तीसगढ़ | कोरकू, भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हल्वा, भतरा, माडिया, सहरिया, कमार, कंवर। |
| त्रिपुरा | लुशाई, माग, हलम, खशिया, भूटिया, मुंडा, संथाल, भील, जमनिया, रियांग, उचाई। |
| जम्मू-कश्मीर | गुर्जर, भरवर वाल। |
| गुजरात | कथोड़ी, सिद्दीस, कोलघा, कोटवलिया, पाधर, टोडिय़ा, बदाली, पटेलिया। |
| उत्तर प्रदेश | बुक्सा, थारू, माहगीर, शोर्का, खरवार, थारू, राजी, जॉनसारी। |
| उत्तरांचल | भोटिया, जौनसारी, राजी। |
| महाराष्ट्र | भील, गोंड, अगरिया, असुरा, भारिया, कोया, वर्ली, कोली, डुका बैगा, गडावास, कामर, खडिया, खोंडा, कोल, कोलम, कोर्कू, कोरबा, मुंडा, उरांव, प्रधान, बघरी। |
| पश्चिम बंगाल | होस, कोरा, मुंडा, उरांव, भूमिज, संथाल, गेरो, लेप्चा, असुर, बैगा, बंजारा, भील, गोंड, बिरहोर, खोंड, कोरबा, लोहरा। |
| हिमाचल प्रदेश | गद्दी, गुर्जर, लाहौल, लांबा, पंगवाला, किन्नौरी, बकरायल। |
| मणिपुर | कुकी, अंगामी, मिजो, पुरुम, सीमा। |
| अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | औंगी आरबा, उत्तरी सेन्टीनली, अंडमानी, निकोबारी, शोपन। |
| केरल | कडार, इरुला, मुथुवन, कनिक्कर, मलनकुरावन, मलरारायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान, उल्लातन, यूराली, विशावन, अर्नादन, कहुर्नाकन, कोरागा, कोटा, कुरियियान,कुरुमान, पनियां, पुलायन, मल्लार, कुरुम्बा। |
| पंजाब | गद्दी, स्वागंला, भोट। |
| राजस्थान | मीणा, भील, गरसिया, सहरिया, सांसी, दमोर, मेव, रावत, मेरात, कोली। |
| सिक्किम | लेपचा। |
भारत की जनजातियों के प्रमुख समस्याएँ
भारत की जनजातियों में आदिम विशेषताएं, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े समुदाय से संपर्क में संकोच और पिछड़ापन की प्रमुख मुद्दे है। परिणामस्वरूप, उन्हें अपने सम्पूर्ण जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
भारत में जनजातीय समस्याएँ निम्नलिखित है:-
(i) सामाजिक समस्याएँ:-
सामाजिक समस्याओं की बात की जाय तो ये आज भी सामाजिक संपर्क स्थापित करने में अपने-आप को सहज नहीं पाते हैं। इस कारण ये सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती हैं।
(ii) धार्मिक समस्याएँ:-
धार्मिक अलगाव भी जनजातियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा पहलू है। इन जनजातियों के प्राय: अपने अलग देवी-देवता होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है समाज में अन्य वर्गों द्वारा इनके प्रति छुआछूत का व्यवहार रखना। अगर हम थोड़ा पीछे जायें तो पाते हैं कि इन जनजातियों को अछूत तथा अनार्य मानकर समाज से बेदखल कर दिया जाता था, सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश तथा पवित्र स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। आज भी इनकी स्थिति ले-देकर यही है।
(iii) शैक्षिक समस्याएँ:-
आज भी जनजातीय समुदायों का एक बहुत बड़ा वर्ग निरक्षर है जिससे ये आम बोलचाल की भाषा को समझ नहीं पाती हैं। सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ इनके लिये हैं इसकी जानकारी तक इनको नहीं हो पाती है जो इनके शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। 2001 से 2011 तक, ST के लिए साक्षरता दर में 11.86 प्रतिशत अंक और पूरी आबादी के लिए 8.15 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखने को मिला है।
(iv) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:-
स्वास्थ्य सेवा के मामले में जनजातीय आबादी के बीच संदिग्ध मुद्दे हैं। सबसे कमजोर कड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में काम करने के लिए इच्छुक, प्रशिक्षित और सुसज्जित स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की कमी जनजातीय आबादी को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण बाधा है। अनुसूचित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और प्रबंधकों के बीच कमी, रिक्तियाँ, अनुपस्थिति या उदासीनता है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नीतियों को आकार देने, योजना बनाने या सेवाओं को लागू करने में अनुसूचित जनजातियों के लोगों या उनके प्रतिनिधियों की भागीदारी का लगभग पूर्ण अभाव, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुचित तरीके से डिजाइन किए गए और खराब तरीके से संगठित और प्रबंधित स्वास्थ्य सेवा के कारणों में से एक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) जैसे चिकित्सा बीमा कवरेज अनुसूचित क्षेत्रों में बहुत कम हैं। इसलिए, जनजातीय लोग भयावह और गंभीर बीमारियों के प्रति सुरक्षा के बिना रहते हैं। जनजातीय लोगों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 44 से 74 के बीच होने का अनुमान है।
(v) आर्थिक समस्याएँ:-
इनके आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात की जाए तो इसमें प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है। आज भी जनजातियों के समुदाय का एक बड़ा तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर अपना जीवनयापन कर रहा है। माँ-बाप आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा नहीं पाते हैं तथा पैसे के लिये उन्हें बड़े-बड़े व्यवसायियों या दलालों को बेच देते हैं। बच्चे या तो समाज के घृणित से घृणित कार्य को अपनाने हेतु विवश हो जाते हैं या तो उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है।
रही बात लड़कियों की तो उन्हें अमूमन वेश्यावृत्ति जैसे घिनौने दलदल में धकेल दिया जाता है। दरअसल जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें उनकी बाकी सुविधाओं से वंचित करता है।
(vi) तम्बाकू और शराब का सेवन:-
एक्सा कमेटी रिपोर्ट 2014 के आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि 15 से 54 वर्ष की आयु के पुरुष काफी अधिक मात्रा में तम्बाकू का सेवन करते हैं, या तो धूम्रपान करते हैं या चबाते हैं। जनजातियों के लगभग 72 % और गैर-जनजातियों के 56 % लोगों में तम्बाकू का सेवन प्रचलित था।
नशाखोरी ने इन आदिवासियों के पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। प्रत्येक आदिवासी परिवार त्योहार, विवाह आदि उत्सवों पर खूब शराब, गांजा, भांग व अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करते है। शराब पीने से उनकी आर्थिक स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।
(vii) गरीबी और ऋणग्रस्तता:-
अधिकांश जनजातियाँ गरीब हैं। जनजातियाँ अल्पविकसित तकनीक पर आधारित कई तरह के सरल व्यवसायों में संलग्न हैं। अधिकांश व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय हैं जैसे- शिकार करना, लकड़ी इकट्ठा करना और कृषि करना।
विभिन्न जनजातियों के 60 प्रतिशत से अधिक परिवार किसी न किसी रूप में ऋणग्रस्त हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह, सामूहिक भोज जैसे अवसरों के लिए ली गई ऋण की राशि द्वारा जनजातीय लोग भारत की सांस्कृतिक धरोहर जनजातियाँ अपने दायित्वों को पूरा करते हैं। यद्यपि सरकार की विभिन्न संस्थाओं आई.टी.डी.ए., सहकारी समितियों, बैंकों व जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा नाममात्र के ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है किन्तु अशिक्षा, अज्ञानता के कारण जनजातीय लोग अपनी जनजाति या महाजनों से ही ऋण लेना पंसद करते हैं। ऋणग्रस्तता के लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं-
⇒ नई वन नीति के कारण वन सम्पदा के उपयोग से वंचित,
⇒ जनजातीय कृषि भूमि का छोटा आकार व अनुपजाऊ होना,
⇒ उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त ना होना,
⇒ खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना,
⇒ मद्यपान व आय से अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति,
⇒ ऋण लेने के लिए सरकारी संस्थाओं की अपेक्षा स्थानीय महाजनों पर निर्भरता।
ऋणग्रस्तता की समस्या के कारण जनजातीय समाज का निरंतर विघटन हो रहा है क्योंकि गरीबी के कारण उचित मात्रा में भोजन का अभाव अनेक रोगों को जन्म देता है। साथ ही चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होने के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं होती। बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और कृषि भूमि से बेदखल होने की समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।
यातायात के साधनों का अभाव:-
अधिकांश जनजातियाँ पहाड़ों, जंगलों और दूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां उनका अन्य लोगों से सम्पर्क नहीं हो पाता क्योंकि आवागमन के साधनों का अभाव है। अतः उन्हें जीवनयापन के उचित अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।
वन सम्पदा पर रोक:-
जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वन सम्पदा जैसे कीमती लकड़ी, फल-फूल, जड़ी-बूटियाँ, चाय बागान आदि प्रचुरता में उपलब्ध हैं जिनके कारण अनेक उद्योगों का विकास हुआ किन्तु इसका दुष्प्रभाव दो रूपों में पड़ा। बाह्य लोगों जैसे व्यापारी, महाजन, ठेकेदार, प्रशासक, पुलिस अधिकारियों के साथ समायोजन व्यवहार की समस्या तथा इनकी गरीबी व अशिक्षा का लाभ उठाकर बाह्य लोगों द्वारा इनका शोषण किया गया।
प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर रोक:-
ब्रिटिश शासन से पूर्व ये जनजातियां राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र इकाइयां थीं। वन खनिज संपदा पर इनका एकाधिकार था किन्तु अंग्रेजों द्वारा सम्पूर्ण देश में एक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित कर जनजातियों के अधिकार सीमित कर दिए गए और प्राकृतिक सम्पदा के उपभोग पर रोक लगा दी गई। नई प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था से संतुलन बनाने में जनजातीय समाज को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
धर्म परिवर्तन की समस्या:-
ब्रिटिश शासनकाल में ही ईसाई मिशनरियों द्वारा उनके विकास, कल्याण के नाम पर आर्थिक प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कर ईसाई बनाया गया जिसके फलस्वरूप अनेक आर्थिक व परसंस्कृति ग्रहण सम्बम्धी समस्याओं का विकास हुआ। मजूमदार तथा मदन के अनुसार भारतीय जनजातियों की अधिकांश समस्याएं उनके भौगोलिक पृथक्करण और नए सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम हैं।
जनजातियों के उत्थान के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम
भारतीय संविधान में जहाँ एक ओर अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है तो वहीं दूसरी ओर, अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उपबंध भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 समाज में किसी भी तरह की अस्पृश्यता का निषेध करता है तो नीति निदेशक तत्त्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे।
जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-
शिक्षा
(i) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की स्थापना करके दूर-दराज के इलाकों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।
(ii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) और राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं।
(iii) आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाती है।
आर्थिक विकास
(ii) प्रधानमंत्री पीवीटीजी (Particularly Vulnerable Tribal Groups) विकास मिशन के तहत, कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम किया जाता है।
सामुदायिक स्थिरता
(i) आदिवासी भूमि और संस्कृतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
(ii) आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना की जाती है।
(iii) आदिवासी महिलाओं और लड़कियों में साक्षरता के स्तर में अंतर को कम करने का काम किया जाता है।
इनके अलावा, ग्राम पंचायतों और लोकसभाओं, विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।