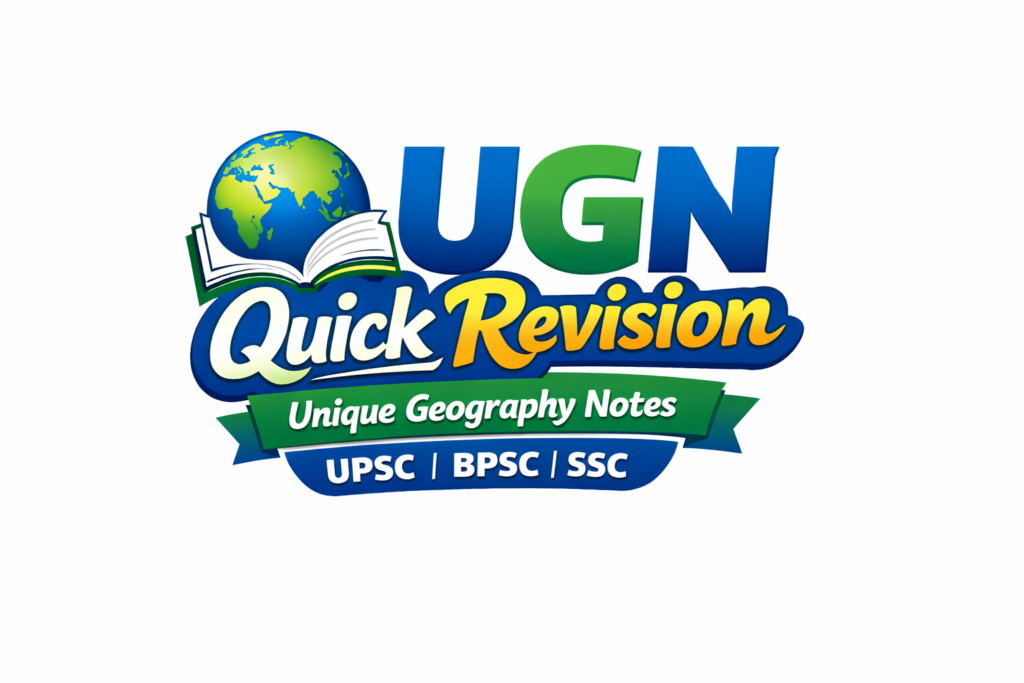28. Non-Conventional Sources of Energy (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोत)
Non-Conventional Sources of Energy
(ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोत)

ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्त्रोत वे हैं जो प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय होते हैं तथा जिनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। जैसे- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, बायोमास, भू-तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, लहर ऊर्जा आदि।
ये स्रोत पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं और पारंपरिक स्रोतों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करते हैं।
आज विकासशील देशों में बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण जीवाश्म ईंधन संसाधन जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा एक सीमित संसाधन के रूप में रह गये हैं।
ब्रून्श ने तो कोयला और खनिज तेल को लुटेरा संसाधन बताया है। वह दिन दूर नहीं है जब विश्व में इन संसाधनों के संचित भण्डार समाप्त हो जायेंगे। इसी डर के कारण आज विश्व के देश ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोतों पर निर्भर रहने लगे हैं।
ऊर्जा के इन स्त्रोंतों का प्रयोग होने से न केवल जीवाश्म ईंधन की बचत होगी वरन् बहुत कुछ विदेशी मुद्रा भी बचेगी।
(i) सौर ऊर्जा (Solar Energy):-
यद्यपि सौर ऊर्जा विश्व के सभी देशों में उपलब्ध है परन्तु सौर ऊर्जा की सर्वाधिक सम्भावता उष्ण कटिबंधीय देशों में है जहाँ सूर्य की किरणें सालोंभर अधिक तेज पड़ती हैं। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण बढ़ने के बाद सूर्यातप कम होने लगता है।
सबसे अधिक सूर्याताप की सम्भावना मरूस्थलीय क्षेत्रों में होती है। सूर्य की किरणों से ऊर्जा तब प्राप्त होती है जब सीधी किरणें फोटो-वोल्टिक सैल (Photo-Voltaic-Cells) से टकराती हैं फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस विधि द्वारा ऊर्जा दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है-
(i) फोटोवोल्टिक ऊर्जा इस विधि द्वारा ऊर्जा सूर्य की किरणों से (Semi-conductor device) द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन इस विधि द्वारा उत्पन्न ऊर्जा काफी महँगी पड़ती है। आज अनेक शोधों द्वारा फोटो वोल्टिक विधि से ऊर्जा बनाने की विधि को सस्ता किया गया है।
इस विधि से सौर की किरणों को बड़े-बड़े आतिशी शीशों, लेंसों अथवा रिफ्लेक्टरों की सहायता से बड़ी मात्रा में एकत्र किया जाता है।
(ii) दूसरी विधि से सौर ऊर्जा से सीधे विद्युत बनाई जाती है। इसके लिये विभिन्न प्रकार के सिलिकॉन सैलों का प्रयोग किया जाता है।
ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्त्रोतों में विश्व ऊर्जा का 0.5% सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा के उत्पादन की सम्भावनाएँ भारत और चीन में पर्याप्त हैं। यहाँ सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने, सौर कुकर बनाने तथा फसल पकाने आदि की तकनीकी विकसित की जा चुकी है।
भारत-
यहाँ सौर ऊर्जा के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। ऊर्जा मंत्रालय ने 25 से 100 kW की तीन प्रकार की सौर फोटो-वोल्टिक ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की हैं-
(i) सार्वजनिक भवनों की छत पर प्रणाली लगाना ताकि प्रमुख शहरी क्षेत्रों में पीक लोडिंग सेविंग हो सके।
(ii) सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड के अन्तिम भाग के लिये ही एण्ड स्पोर्ट प्रणाली की व्यवस्था।
(iii) दूर दराज क्षेत्रों में डीजल की बचत करने वाला लगाना।
भारत में राजस्थान के जोधपुर जिले में 140 MW की एक समन्वित सौर शक्ति संयुक्त चक्र बिजली सहित 35 MW की ताप ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव भी है। भारतवर्ष में 10 ग्रिड इंसेंटिव एस. पी. वी. परियोजनाएँ लगाई जा रही हैं जिनकी कुल क्षमता 925 kW है।
चीन-
यहाँ सौर ऊर्जा से लगभग 20,000 Heat Collectors तैयार किये जाते हैं।
सौर ऊर्जा की ओर विश्व के अन्य देश जैसे श्रीलंका, इण्डोनेशिया, यू. एस. ए. प्रयत्नशील हैं। यू एस. ए. में तो कैलीफोर्निया में 600 MW का एक संयंत्र स्थापित किया गया।
वैज्ञानिकों की योजना है कि सूर्यातप को इस्पात नलिकाओं में एकत्रित करके आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। इसके लिये नलिकाओं में नाइट्रोजन प्रवाह करना होगा, जो इस ताप को गलित लवणों के टैंकों में परिवहित कर देंगी। यह टैंक बहुत दिनों तक ताप को बनाये रखते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसे टरबाइन जेनरेटर और परम्परागत बायलर में विद्युत उत्पादन के लिये प्रयोग किया जा सकेगा।
आज अन्तरिक्ष उपग्रहों का भी सहयोग इसके लिये लिया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलीफोर्निया और फ्लोरिडा में वाणिज्यिक स्तर पर सौर हीटरों का प्रचलन है। सौर कुकर, हीटर, ड्रायर, सिलिकन आदि सौर तापीय उपकरण विकसित किये गये हैं।
विश्व की विषालतम सौर भट्टी लॉस एंजिलिस से 140 मील उत्तर-पूर्व की ओर है। यह मोजाब मरूस्थल में लूज में स्थापित है। इससे 10 विशाल सौर विद्युत उत्पादक संयंत्र संचालित होते हैं।
(ii) पवन ऊर्जा (Wind Energy):-
पवन ऊर्जा, जिसे विंड एनर्जी भी कहते हैं। इसमें हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है।
पवन चक्कियों का प्रयोग ऊर्जा के रूप में बहुत समय से किया जा रहा है। ईरान में अन्न पीसने के लिये पहले पवन चक्कियों का प्रयोग होता है। इंग्लैण्ड में हल के निकट सन् 1186 में पवन चक्कियाँ स्थापित की गई थीं। आज हालैण्ड में पवन चक्कियों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। इंग्लैण्ड की सबसे पुरानी पवन चक्की सन् 1670 की आज भी स्थित है।
इस विधि द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने में पवन द्वारा गतिज (Kinetic) ऊर्जा का प्रयोग टरबाइन के माध्यम से विद्युत उत्पादन में होता है।
पवन द्वारा ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक जर्मनी में होता है। यहाँ सन् 2000 तक 9.369 पवन टरबाइन लगे हुए थे जिनसे 6,094.8 MW विद्युत उत्पादन होता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। यहाँ सन् 1999 तक 2,502 MW पवन ऊर्जा का उत्पादन हुआ। किसी समय तो अमेरिका के पश्चिमी मैदान में जल की पंपिंग के लिए पवन चक्की का प्रयोग होता था। यहाँ अधिकतर पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्र कैलीफोर्निया राज्य में हैं। यहाँ लगभग 15,000 टरबाइन ऊर्जा उत्पादन में कार्यरत हैं। जबकि डेनमार्क विश्व में तीसरा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ सन् 2000 तक 2,417 MW विद्युत का उत्पादन हुआ।
ग्रेट ब्रिटेन यहाँ सन् 2001 में 69 पवन फार्म थे जिनमें 941 टरबाइन लगे हुए थे तथा इनमें 473.6 MW विद्युत उत्पादित होती है।
भारत भी पवन ऊर्जा के उत्पादन में पीछे नहीं हैं। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है। भारत में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2023 में 42.633 गीगावाट थी, और देश दुनिया में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है।
एशिया की विशालतम 150 MW उत्पादन क्षमता परियोजना मुप्पंडाल (तमिलनाडु) में है। इस समय देश में 179 विण्ड मैपिंग और 83 विण्ड मोनीटरिंग स्टेशन कार्यरत हैं। तामिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में लगभग 80 स्थानों की पहचान की जा चुकी है।
(iii) भूतापीय शक्ति (Geo-thermal Energy):-
पृथ्वी के आन्तरिक भाग में गहराई के अनुसार तापमान में वृद्धि होती है। ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान 4,500°C है जहाँ पर लोहा तथा निकिल जैसे भारी धात्विक पदार्थ भी तरल अवस्था में हैं।
पृथ्वी की परत के धरातल पर दरार पड़ने के कारण मैग्मा बाहर आ जाता है। इसके ताप को एकत्रित करके विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। यही विद्युत उत्पादन भूतापीय शक्ति कहलाता है।
विशेषज्ञों का मत है कि इस ऊर्जा का उपयोग कूप खोदकर तथा शीत जल को पम्प द्वारा इस विभंगित शैल में प्रवाहित किया जाता है यह जल शैल की ऊष्मा से 350°F तक गर्म होकर संवहन द्वारा धरातल की ओर, को उठेगा, तब इसकी ऊर्जा को टरबाइनों में चलाने के लिये प्रयोग किया जायेगा।
एक अन्य विचारधारा के अनुसार भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लिये दो कूपों (Shafts) को बनाया जाए। एक कूप जल को पम्प से नीचे की ओर भेजेगा जब जल अत्याधिक गर्म हो जायेगा तो दूसरे कूप से इसे ऊपर खींच लिया जायेगा और विद्युत शक्ति के उत्पादन में प्रयोग किया जायेगा।
भूतापीय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त एवं सस्ती होती है। न्यूजीलैण्ड, आइसलैण्ड और इटली में प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग काफी पहले से किया जा रहा है। इटली के ट्यूस्केनी प्रान्त में फ्लोरेन्स के दक्षिण-पश्चिम में लारडेरेल्लो का प्राकृतिक वाष्प क्षेत्र सन् 1913 से विद्युत उत्पादन कर रहा है।
भारतवर्ष में भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा देश भर में 340 भूतापीय गर्म झरनों की पहचान कर ली गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में तातापानी भूतापीय क्षेत्रों में 300 kW क्षमता का भूतापीय बिजली संयंत्र लगाने की मंजुरी दी गई है।
इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर में पूगा, भूतापीय क्षेत्रों में जलाशय की क्षमता का मूल्यांकन करने तथा बिजली संयंत्र लगाने की संभाव्यता की जाँच का काम राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा किया गया है।
कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में मणिवर्ण स्थान पर भूतापीय ऊर्जा पर आधारित एक कोल्ड स्टोरेज और एक बिजलीघर स्थापित किया गया है।
(iv) ज्वारीय ऊर्जा (Tidal Energy):-
ज्वारीय ऊर्जा, जिसे टाइडल एनर्जी भी कहा जाता है, समुद्र के ज्वार-भाटे के प्राकृतिक उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप है।
वर्तमान समय में ज्वार ऊर्जा द्वारा भी विश्व के कई देशों में विद्युत उत्पादन किया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम ज्वार ऊर्जा उत्पादक प्लाण्ट फ्रांस के ब्रिटनी में रेन्स नदी की एस्चुअरी पर स्थापित किया गया। इनमें ब्रिटेनी तट पर समुद्री टरबाइन लगे हैं जो ज्वार शक्ति से चालित होते हैं।
इसी प्रकार कनाडा के न्यू ब्रुसविक और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन राज्य में पुंडी की खाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ ज्वार 10 से 25 मीटर तक ऊँचे उठते हैं। ज्वार शक्ति से विद्युत उत्पादित की जाती है।
रूस की किशलाया खाड़ी में भी इसी प्रकार के प्लाण्ट स्थापित किये गये हैं, भारतवर्ष में खम्भात की खाड़ी तथा सुन्दरवन इसके संभावित क्षेत्र हैं। यहाँ उत्पादित क्षमता 8,000-9,000 kW तक है।
(v) शहरी और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा (Energy from Urban and Industrial Waste):-
नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कूड़े-कचरे से पर्यावरण दूषित होता है। इस कूड़े-कचरे का उपचार करके न केवल पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है वरन् ऊर्जा उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। बड़े-बड़े महानगरों में यह कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है।
इस ऊर्जा से विद्युत के साथ-साथ गैस भी उत्पादित की जा सकती है। भारतवर्ष में सन् 1995 से शहरी, नगरपालिका और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है।
(vi) बायोमास ऊर्जा (Biogas Energy):-
इसके अन्तर्गत कृषि और वन्य अवशेषों का उपयोग किया जाता है। इससे विद्युत के अतिरिक्त गैस भी उत्पन्न की जाती है। भारतवर्ष में बायोमास गैसीय कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक उपयोगों के लिए ताप ऊर्जा उत्पन्न करने, पानी की पंपिंग और 500 kW तक बिजली पैदा करने के लिये बायोमास गैसीफायर विकसित किये गये हैं।
इन गैसीफायर में लकड़ी के टुकड़ों और दूसरी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष में 53.1 मेगावाट की क्षमता के बायोमास, गैसीफायर अब तक विकसित किये जा चुके हैं।
इसके अतिरिक्त नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत फ्यूज सेल्स, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के बीच अभिक्रिया के जरिये बिजली पैदा होती है।
हाइड्रोजन ऊर्जा, इसका प्रयोग व्यापक रूप से जीवाश्म ईंधन के रूप में किया जाता है। जैव ईंधन आदि का प्रयोग भी विद्युत उत्पादन में किया जाता है।