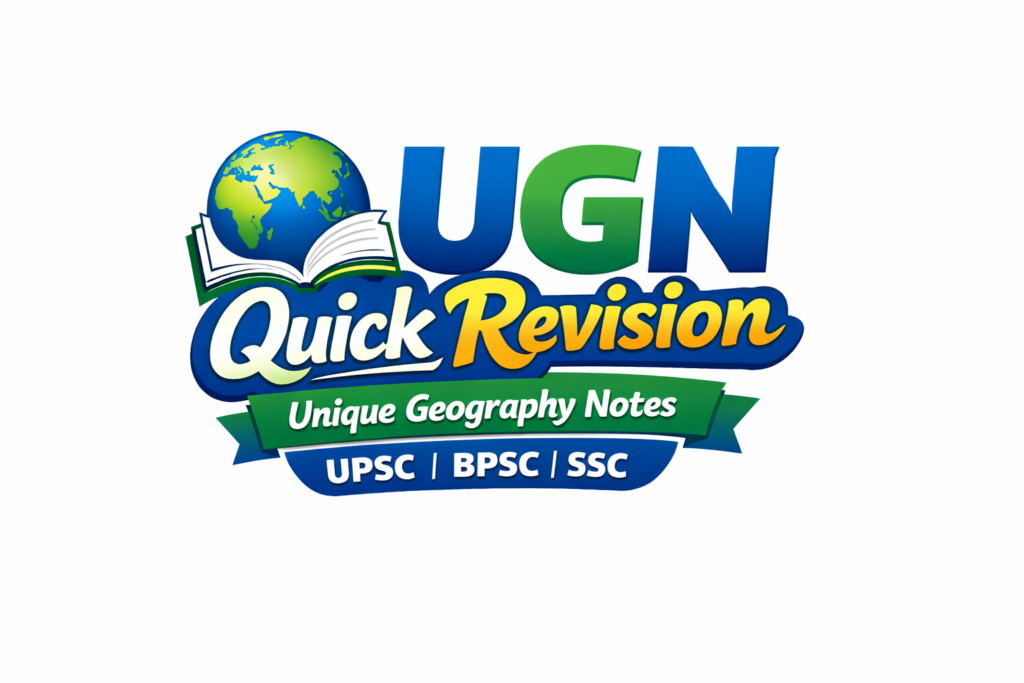32. Natural disaster: Drought, Flood and Earthquake (प्राकृतिक आपदाएँ: सूखा, बाढ़ और भूकंप)
Natural disaster: Drought, Flood and Earthquake
(प्राकृतिक आपदाएँ: सूखा, बाढ़ और भूकंप)

परिचय
प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन के लिए एक गंभीर चुनौती हैं। ये ऐसी घटनाएँ हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण अचानक घटित होती हैं और जिनका प्रभाव पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था तथा जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ता है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति के बावजूद मानव आज भी प्रकृति के प्रकोपों से पूर्णतः सुरक्षित नहीं हो पाया है।
सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएँ न केवल भौतिक विनाश करती हैं बल्कि मानव जीवन की संरचना, संसाधनों और विकास प्रक्रिया को भी बाधित करती हैं। भारत जैसे विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में इन आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता दोनों अत्यधिक हैं।
1. सूखा (Drought)
भारतीय मौसम आयोग (IMO) ने सूखा को परिभाषित करते हुए बतलाया है की मई माह के मध्य से अक्टूबर माह के मध्य लगातार 4 सप्ताह तक वर्षा की मात्रा 5 सेमी० या उससे कम हो, सूखा की स्थिति कहलाएगी। यही समयावधि मानसून के आगमन का है, इसीलिए इसे सूखा का पैमाना बनाया गया है। यानी मानसून के कमजोर होने पर सूखा की स्थिति लगभग तय है।
अर्थात सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके परिणामस्वरूप भूमि की नमी घट जाती है, फसलें नष्ट हो जाती हैं, जलस्रोत सूख जाते हैं और पशु-पक्षी तथा मनुष्य दोनों ही जीवन संकट में पड़ जाते हैं।
सूखे के प्रकार
(i) मौसमी सूखा (Meteorological Drought):-
जब किसी क्षेत्र में औसत वर्षा से 25% या अधिक कमी हो जाती है, तो इसे मौसमी सूखा कहते हैं।
(ii) कृषि सूखा (Agricultural Drought):-
जब मिट्टी की नमी इतनी कम हो जाती है कि फसलों की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होता है।
(iii) जलवैज्ञानिक सूखा (Hydrological Drought):-
जब जलाशयों, नदियों, तालाबों और भूजल स्तर में असामान्य कमी हो जाती है।
(iv) सामाजिक-आर्थिक सूखा (Socio-economic Drought):-
जब सूखे के कारण मानव जीवन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं।
सूखे के कारण
⇒ अनियमित या असमान वर्षा वितरण
⇒ वनों की कटाई और भूमि का अत्यधिक दोहन
⇒ जल संसाधनों का अनुचित प्रबंधन
⇒ जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग
⇒ भूजल का अत्यधिक दोहन
सूखे के प्रभाव
(i) कृषि पर प्रभाव:-
फसलों की उपज घट जाती है, पशुधन मर जाते हैं और खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है।
(ii) सामाजिक प्रभाव:-
पलायन, बेरोजगारी, गरीबी और भूखमरी जैसी स्थितियाँ बढ़ती हैं।
(iii) पर्यावरणीय प्रभाव:-
भूमि बंजर हो जाती है, वनस्पतियाँ सूख जाती हैं और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है।
(iv) आर्थिक प्रभाव:-
किसानों की आय घटती है, उत्पादन लागत बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सूखा प्रबंधन
⇒ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
⇒ सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती
⇒ वनीकरण और भूमि संरक्षण
⇒ सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली
⇒ सरकार द्वारा राहत पैकेज और रोजगार योजनाएँ (जैसे मनरेगा)
2. बाढ़ (Flood)
राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार “बाढ़ वह स्थिति है जब नदी का जल खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है।” खतरे का निशान स्तर 50 वर्षों के औसत प्रवाह का स्तर है। संपूर्ण भारत में 80 नदियों के जलस्तर के गहन अध्ययन के बाद खतरे का निशान का निर्धारण किया गया है।
अर्थात बाढ़ वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह अपनी सामान्य सीमाओं को पार कर मानव बस्तियों, कृषि भूमि और सड़कों को डुबो देती है। यह सबसे सामान्य और व्यापक प्राकृतिक आपदा है।
बाढ़ के प्रकार
(i) नदी बाढ़:
जब नदियाँ अपने तटों से बाहर निकल जाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि की बाढ़।
(ii) शहरी बाढ़:-
जब शहरों में जल निकासी की कमी के कारण वर्षा जल जमा हो जाता है।
(iii) फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़):-
पहाड़ी क्षेत्रों में तीव्र वर्षा या ग्लेशियर पिघलने से अचानक उत्पन्न बाढ़।
(iv) तटीय बाढ़:-
चक्रवात या समुद्री तूफानों के कारण समुद्र का जल तटवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है।
बाढ़ के कारण
⇒ अत्यधिक वर्षा और बादलों का फटना
⇒ नदियों का तल भर जाना और अवैध अतिक्रमण
⇒ जल निकासी प्रणाली का अभाव
⇒ वनों की कटाई और भूमि का क्षरण
⇒ बांधों या तटबंधों का टूटना
बाढ़ के प्रभाव
(i) मानव जीवन पर प्रभाव:-
जन-धन की हानि, बीमारियों का फैलाव, विस्थापन और पलायन।
(ii) कृषि पर प्रभाव:-
फसलों का नष्ट होना, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का बह जाना।
(iii) आर्थिक प्रभाव:-
बुनियादी ढाँचे, सड़कें, पुल, घर आदि का भारी नुकसान।
(iv) पर्यावरणीय प्रभाव:-
जल प्रदूषण, मृदा अपरदन और जैव विविधता पर विपरीत असर।
बाढ़ प्रबंधन उपाय
⇒ बांध, नहरें और तटबंध निर्माण
⇒ वर्षा जल संचयन और जल निकासी सुधार
⇒ नदी तटों पर निर्माण प्रतिबंध
⇒ सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली
⇒ पुनर्वास और राहत कार्य
भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण नीति (National Flood Control Programme) के तहत कई योजनाएँ लागू की हैं, जैसे – गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि।
3. भूकंप (Earthquake)
भूकंप पृथ्वी की सतह के भीतर स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी घर्षण या टकराव के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक आपदा है। इसमें धरती की सतह अचानक हिलने लगती है, जिससे इमारतें, पुल, सड़कें और जनजीवन प्रभावित होता है।
भूकंप के प्रकार
(i) टेक्टोनिक भूकंप:-
पृथ्वी की प्लेटों की गति और टकराव के कारण उत्पन्न होते हैं। ये सबसे सामान्य और शक्तिशाली होते हैं।
(ii) ज्वालामुखीय भूकंप:-
ज्वालामुखी विस्फोट के साथ उत्पन्न होने वाले भूकंप।
(iii) संवेदनशील भूकंप (Collapse Earthquake):-
भूमिगत खानों या गुफाओं के धंसने से उत्पन्न।
(iv) कृत्रिम भूकंप:-
विस्फोट या परमाणु परीक्षणों के कारण होने वाले भूकंप।
भूकंप की तीव्रता का मापन
भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल और मर्काली स्केल से मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर 2 से कम भूकंप सामान्य होता है जबकि 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी होता है।
भूकंप के प्रभाव
भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो पृथ्वी की सतह के भीतर ऊर्जा के अचानक विस्फोट के कारण होती है। इसके प्रभाव व्यापक और विनाशकारी होते हैं।
सबसे पहले, भूकंप से इमारतें, पुल, सड़कें और अन्य संरचनाएँ ढह जाती हैं, जिससे भारी जन-धन की हानि होती है।
भूकंप के कारण भूमिगत पाइपलाइनें टूट जाती हैं, जिससे गैस और पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। कई बार आग लगने और विस्फोट जैसी घटनाएँ भी होती हैं।
भूकंप से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन (landslide) की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे सड़कें और गाँव नष्ट हो जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में यह सुनामी (tsunami) का रूप ले सकता है, जो समुद्री लहरों के रूप में तटीय बस्तियों को पूरी तरह डुबो देती है।
सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी इसके गहरे प्रभाव पड़ते हैं- लोग बेघर हो जाते हैं, रोजगार के साधन नष्ट हो जाते हैं, तथा प्रभावित क्षेत्रों में भय और असुरक्षा का माहौल फैल जाता है।
इसके अतिरिक्त, भूकंप पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। नदियों का मार्ग बदल सकता है और भूमिगत जल स्रोतों में परिवर्तन आ सकता है। अतः भूकंप न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है।
भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र
भारत को पाँच भूकंपीय जोनों में बाँटा गया है-
⇒ जोन V : अत्यधिक संवेदनशील (जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर-पूर्वी राज्य)
⇒ जोन IV : उच्च संवेदनशील (दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश)
⇒ जोन III : मध्यम (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश)
⇒ जोन II एवं I : कम संवेदनशील क्षेत्र
भूकंप प्रबंधन
⇒ भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण
⇒ आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और पूर्व चेतावनी प्रणाली
⇒ सुरक्षित निकासी मार्ग और राहत केंद्र
⇒ जनजागरूकता अभियान
भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन
भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) लागू किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन किया गया है।
इसके अतिरिक्त-
⇒ प्रत्येक राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA)
⇒ जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कार्यरत हैं।
इन संस्थाओं का कार्य आपदा पूर्व तैयारी, राहत एवं पुनर्वास कार्यों का संचालन तथा जन-जागरूकता बढ़ाना है।
निष्कर्ष:-
इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएँ मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनके प्रभाव को वैज्ञानिक तकनीक, सुविचारित नीति और जनसहभागिता से अवश्य कम किया जा सकता है। सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएँ हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर ही सतत् विकास संभव है।
जल संरक्षण, वनीकरण, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन शिक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से हम इन आपदाओं के दुष्प्रभावों को न्यूनतम कर सकते हैं। अतः आवश्यकता है कि हम “आपदा को आपदा न बनने दें, बल्कि उसे सीख और सुधार का अवसर बनाएँ।”