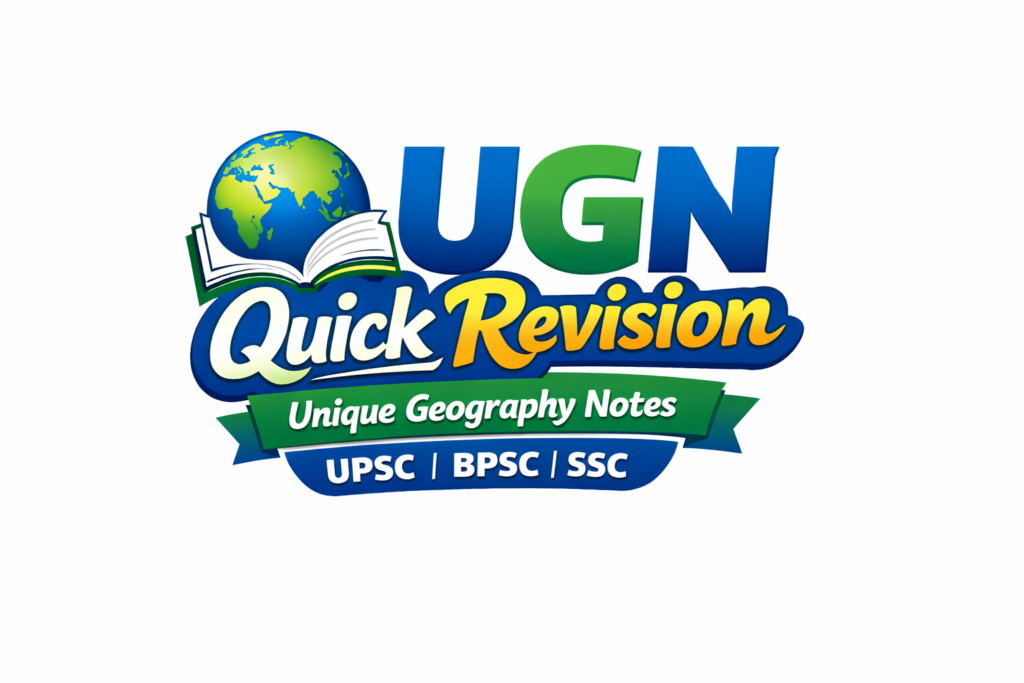33. International Standard of Drinking Water (पेयजल के अंतरराष्ट्रीय मानक)
International Standard of Drinking Water
(पेयजल के अंतरराष्ट्रीय मानक)

परिचय
जल जीवन का मूल स्रोत है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए जल का शुद्ध एवं सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। मानव शरीर का लगभग 70 प्रतिशत भाग जल से निर्मित है, अतः इसका सेवन शुद्ध, स्वच्छ तथा रोगाणु रहित होना चाहिए।
किंतु आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण जल प्रदूषण की समस्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में यह आवश्यक हो गया कि पेयजल के लिए कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए जाएँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित जल मिल सके।
इसी उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization – WHO) तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने पेयजल की गुणवत्ता से संबंधित मानक निर्धारित किए हैं, जिन्हें “अंतरराष्ट्रीय पेयजल मानक (International Drinking Water Standards)” कहा जाता है।
परिभाषा
पेयजल (Drinking Water) वह जल है जो मनुष्य द्वारा पीने, भोजन तैयार करने तथा घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त हो। यह जल भौतिक, रासायनिक और जैविक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। इसमें कोई हानिकारक तत्व, सूक्ष्मजीव या प्रदूषक नहीं होना चाहिए जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करें।
अंतरराष्ट्रीय पेयजल मानकों की आवश्यकता
(i) स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु – दूषित जल अनेक जलजनित रोगों जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिश, हेपेटाइटिस आदि का कारण बनता है।
(ii) वैज्ञानिक तुलना हेतु – विभिन्न देशों में जल की गुणवत्ता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने हेतु।
(iii) विकासशील देशों में नीति निर्माण हेतु – स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों और योजनाओं में दिशा देने हेतु।
() औद्योगिक नियंत्रण हेतु – उद्योगों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट से जल स्रोतों की रक्षा करने हेतु।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के पेयजल मानक
WHO ने अपने “Guidelines for Drinking-water Quality” में पेयजल के लिए विभिन्न मानदंड निर्धारित किए हैं, जो मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटे गए हैं –
1. भौतिक मानक (Physical Standards)
2. रासायनिक मानक (Chemical Standards)
3. जैविक मानक (Biological Standards)
भौतिक मानक (Physical Standards)
भौतिक मानक जल के बाह्य गुणों से संबंधित होते हैं जैसे रंग, गंध, स्वाद, तापमान, और मटमैलापन।
| मानक तत्व | WHO अनुशंसित सीमा | विवरण |
| रंग (Colour) | 15 TCU (True Colour Unit) से अधिक नहीं | अधिक रंग होने पर जल अस्वच्छ प्रतीत होता है। |
| गंध (Odour) | अप्रिय गंध नहीं होनी चाहिए | जैविक या रासायनिक पदार्थों के कारण गंध उत्पन्न होती है। |
| स्वाद (Taste) | सामान्य और प्राकृतिक होना चाहिए | क्लोरीन या अन्य रसायनों की अधिकता स्वाद को प्रभावित करती है। |
| मटमैलापन (Turbidity) | 5 NTU से कम | अधिक मटमैलापन रोगाणुओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। |
| तापमान (Temperature) | 25°C से कम | अधिक तापमान वाले जल का स्वाद खराब हो जाता है। |
रासायनिक मानक (Chemical Standards)
रासायनिक मानक जल में उपस्थित विभिन्न रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों की सीमा निर्धारित करते हैं। इन तत्वों की अधिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।
| तत्व | स्वीकार्य सीमा (WHO) | प्रभाव |
| pH मान | 6.5 – 8.5 | बहुत अम्लीय या क्षारीय जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। |
| कुल घुलित ठोस (TDS) | 500 mg/L | स्वाद और उपयोगिता पर प्रभाव डालता है। |
| क्लोराइड (Chloride) | 250 mg/L | अधिक मात्रा में खारापन बढ़ाता है। |
| सल्फेट (SO₄) | 250 mg/L | अधिक मात्रा दस्त या उल्टी का कारण बन सकती है। |
| नाइट्रेट (NO₃) | 50 mg/L | बच्चों में “ब्लू बेबी सिंड्रोम” का कारण बनता है। |
| फ्लोराइड (F⁻) | 1.0 mg/L | कम मात्रा में दाँतों के लिए लाभदायक, अधिक मात्रा में फ्लोरोसिस। |
| आयरन (Fe) | 0.3 mg/L | अधिक मात्रा जल का स्वाद बदलती है, पाइपों में जंग लगाती है। |
| मैंगनीज (Mn) | 0.1 mg/L | तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। |
| आर्सेनिक (As) | 0.01 mg/L | कैंसरजनक तत्व, दीर्घकालीन सेवन से त्वचा रोग। |
| सीसा (Pb) | 0.01 mg/L | तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुँचाता है। |
| पारा (Hg) | 0.001 mg/L | गुर्दों और मस्तिष्क को नुकसान। |
| कैडमियम (Cd) | 0.003 mg/L | हड्डियों और किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव। |
जैविक मानक (Biological Standards)
जल में उपस्थित सूक्ष्मजीव रोगों के प्रमुख स्रोत हैं। अतः WHO ने जैविक मानकों के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं।
| सूक्ष्मजीव | WHO अनुशंसा |
|---|---|
| E. coli (Escherichia coli) | 0 प्रति 100 ml जल में |
| कोलीफॉर्म बैक्टीरिया | 0 प्रति 100 ml |
| वायरस, प्रोटोजोआ, हेल्मिंथ्स | अनुपस्थित होने चाहिए |
यदि जल में उपर्युक्त किसी भी प्रकार के रोगाणु पाए जाते हैं, तो वह पेयजल के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।
भारत में पेयजल मानक (BIS – IS 10500:2012)
भारत में पेयजल की गुणवत्ता मानक भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये मानक अधिकांशतः WHO के दिशा-निर्देशों पर आधारित हैं।
| तत्व | स्वीकार्य सीमा | अधिकतम अनुमेय सीमा |
| pH | 6.5 – 8.5 | – |
| कुल कठोरता (Hardness) | 200 mg/L | 600 mg/L |
| TDS | 500 mg/L | 2000 mg/L |
| फ्लोराइड | 1.0 mg/L | 1.5 mg/L |
| नाइट्रेट | 45 mg/L | – |
| आयरन | 0.3 mg/L | – |
| आर्सेनिक | 0.01 mg/L | – |
| सीसा | 0.01 mg/L | – |
भारत सरकार द्वारा “जल जीवन मिशन”, “स्वच्छ भारत मिशन”, और “राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम” के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अंतरराष्ट्रीय मानकों के अन्य संगठन
1. यूएस एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (USEPA) – अमेरिका में पेयजल की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करती है।
2. यूरोपीय संघ (European Union Drinking Water Directive) – यूरोपीय देशों के लिए गुणवत्ता मानक तय करता है।
3. ISO (International Organization for Standardization) – जल गुणवत्ता के मापदंडों के लिए तकनीकी दिशा-निर्देश प्रदान करता है (ISO 10500 आदि)।
4. FAO/UNESCO संयुक्त आयोग – जल संसाधनों के संरक्षण और गुणवत्ता मानकों पर कार्य करता है।
पेयजल गुणवत्ता के मूल्यांकन के प्रमुख पैरामीटर
(i) भौतिक पैरामीटर – रंग, गंध, मटमैलापन, तापमान।
(ii) रासायनिक पैरामीटर – pH, TDS, नाइट्रेट, फ्लोराइड, भारी धातुएँ।
(iii) जैविक पैरामीटर – बैक्टीरिया, वायरस आदि।
(iv) रेडियोधर्मी पदार्थ – ट्रिटियम, रेडियम आदि की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।
पेयजल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत
⇒ औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक कारखाने।
⇒ कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और उर्वरक।
⇒ घरेलू सीवेज और अपशिष्ट जल।
⇒ भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड या नाइट्रेट की प्राकृतिक अधिकता।
⇒ असुरक्षित जल भंडारण और पाइपलाइन लीक।
पेयजल की गुणवत्ता सुधार के उपाय
(i) जल का शोधन (Treatment)- क्लोरीनीकरण, उबालना, फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस (RO)।
(ii) स्रोत संरक्षण – नदी, झील, भूमिगत जल स्रोतों का प्रदूषण से बचाव करना।
(iii) जनजागरूकता – स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति लोगों को शिक्षा देना।
(iv) नियमित परीक्षण – समय-समय पर जल की गुणवत्ता की जांच करना।
(v) नीति निर्माण – सरकार द्वारा कठोर मानक और निगरानी तंत्र की स्थापना करना।
निष्कर्ष:
पेयजल के अंतरराष्ट्रीय मानक मानव स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। WHO और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि जल में किसी भी प्रकार का रासायनिक, जैविक या भौतिक प्रदूषण मानव जीवन को प्रभावित न करे।
भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इन मानकों का पालन करना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रश्न है बल्कि सतत विकास का भी आधार है। इसलिए प्रत्येक नागरिक, संस्था और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को स्वच्छ, सुरक्षित और मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो।