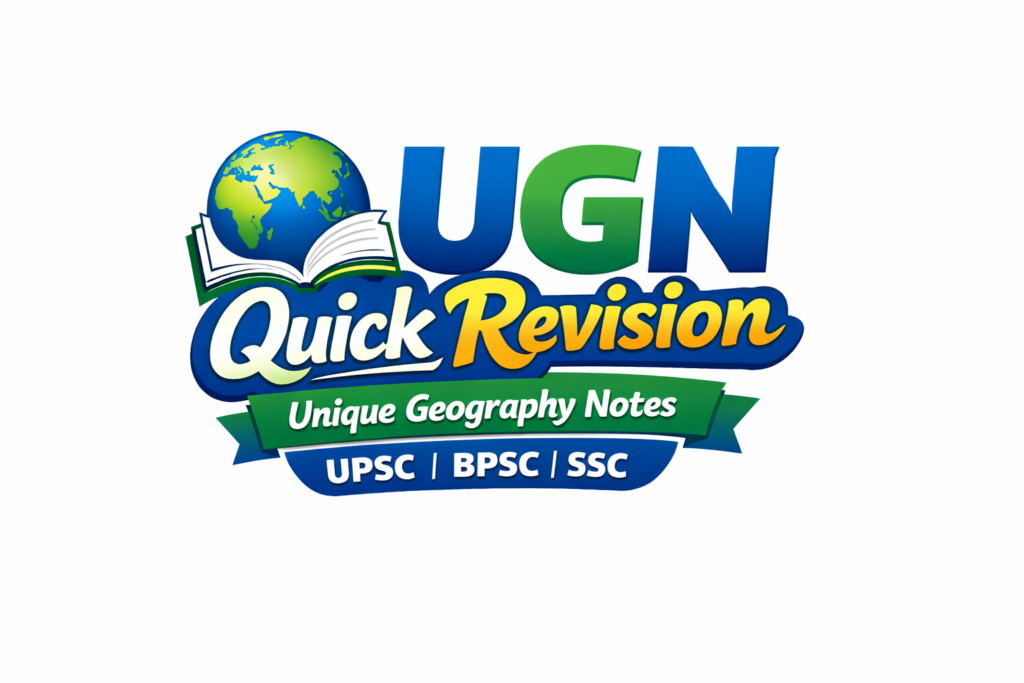24. Gas leak (गैस रिसाव)
Gas leak
(गैस रिसाव)
गैस आधुनिक जीवन और औद्योगिक विकास का अभिन्न अंग हो गया है। घरेलू स्तर पर खाना बनाने से लेकर औद्योगिक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन, वाहन संचालन, दवा निर्माण, उर्वरक निर्माण और रासायनिक प्रक्रियाओं में गैस का प्रयोग होता है। हलांकि गैस का उपयोग जितना उपयोगी है, उससे जुड़ा खतरा उतना ही गंभीर भी है। यदि गैस का रिसाव (Gas Leakage) हो जाए तो यह दुर्घटनाओं, आग, विस्फोट, स्वास्थ्य-हानि तथा पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बन सकता है। अतः गैस रिसाव एक गंभीर सामाजिक, औद्योगिक और पर्यावरणीय समस्या है, जिस पर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो जाता है।
परिभाषा
गैस रिसाव वह स्थिति है जब किसी पाइपलाइन, सिलेंडर, टैंक या औद्योगिक संयंत्र से गैस अनियंत्रित रूप से बाहर निकलने लगे। यह गैस प्रज्वलनशील (flammable), विषैली (toxic) अथवा दमघोंटू (asphyxiant) हो सकती है। इस तरह का रिसाव सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण तीनों के लिए खतरनाक होता है।
गैस रिसाव के सामान्य स्रोत
गैस रिसाव कई कारणों से हो सकता है। इसके प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं-
1. घरेलू स्तर पर:-
- एलपीजी (Liquefied Petroleum Gas) सिलेंडरों से रिसाव
- चूल्हे या पाइपलाइन में खराबी
- रेगुलेटर व नलियों में दरार
2. औद्योगिक स्तर पर:-
- रासायनिक कारखानों में गैस उत्पादन के दौरान रिसाव
- भंडारण टैंकों या पाइपलाइन में लीकेज
- मशीनरी की खराबी या रखरखाव में लापरवाही
3. परिवहन व वितरण प्रणाली में:-
- गैस टैंकरों से दुर्घटनावश रिसाव
- लंबी पाइपलाइन नेटवर्क में दरारें
- दबाव नियामक (Pressure Regulator) की गड़बड़ी
प्रमुख कारण
गैस रिसाव के पीछे तकनीकी और मानवीय दोनों प्रकार की त्रुटियाँ जिम्मेदार होती हैं।
(i) तकनीकी कारण:-
पाइपलाइन की जंग लगना, उपकरणों की पुरानी स्थिति, सील या जोड़ों की कमजोरी।
(ii) मानवीय त्रुटियाँ:-
कर्मचारियों की लापरवाही, सुरक्षा नियमों का पालन न करना, प्रशिक्षण की कमी।
(iii) प्राकृतिक कारण:-
भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदाओं से पाइपलाइन या टैंक का क्षतिग्रस्त होना।
(iv) अनियमित रखरखाव:-
समय-समय पर निरीक्षण और मरम्मत का अभाव।
गैस रिसाव से होने वाले प्रभाव
गैस रिसाव (Gas Leakage) एक गंभीर समस्या है, जिसका प्रभाव व्यक्ति, समाज और पर्यावरण सभी पर गहरा पड़ता है। इसके प्रभाव तात्कालिक (तुरंत होने वाले) और दीर्घकालिक (लंबे समय तक बने रहने वाले) दोनों हो सकते हैं। नीचे इसके प्रमुख प्रभाव दिए जा रहे हैं:-
तात्कालिक प्रभाव
(i) मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:-
- सिर दर्द, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ
- आंख, नाक व गले में जलन
- अधिक मात्रा में गैस के संपर्क से बेहोशी और मृत्यु
- मिथाइल आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें घातक प्रभाव डाल सकती हैं
(ii) पर्यावरण पर प्रभाव:-
- वायुमंडलीय प्रदूषण
- पौधों और जीव-जंतुओं की मृत्यु
- जल व मिट्टी का प्रदूषण (यदि रिसी हुई गैस रासायनिक हो)
(iii) सामाजिक व आर्थिक प्रभाव:-
- आग लगने से जन-धन की हानि
- बड़े औद्योगिक हादसों से हजारों लोग प्रभावित
- उत्पादन प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर, उद्योग का नुकसान
दीर्घकालिक प्रभाव
-
अगली पीढ़ी पर असर- जहरीली गैसों के कारण जन्म लेने वाले बच्चों में शारीरिक व मानसिक विकलांगता हो सकती है।
-
स्थायी प्रदूषण- प्रभावित क्षेत्र लंबे समय तक प्रदूषित बने रहते हैं।
-
विश्वसनीयता में कमी- दुर्घटना वाले उद्योग और क्षेत्र की छवि खराब हो जाती है, जिससे निवेश और विकास बाधित होता है।
गैस रिसाव से जुड़ी प्रमुख घटनाएँ
(i) भोपाल गैस त्रासदी (1984):-
⇒ भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा।
⇒ यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव।
⇒ लाखों लोग प्रभावित, हजारों की मौत, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ।
(ii) विश्व की अन्य घटनाएँ:-
⇒ जर्मनी, रूस और अमेरिका में कई औद्योगिक गैस विस्फोट।
⇒ हाल के वर्षों में भारत में भी सिलेंडर फटने और टैंकर दुर्घटनाओं की घटनाएँ आम हैं।
गैस रिसाव की पहचान
गैस रिसाव का समय रहते पता लगाना जीवन रक्षक हो सकता है।
(i) गंध से पहचान:-
एलपीजी जैसी गैसों में गंध मिलाई जाती है ताकि रिसाव होने पर तुरंत पता चले।
(ii) झाग परीक्षण:-
पाइप या जोड़ पर साबुन का पानी लगाकर बुलबुले उठने से रिसाव का पता चलता है।
(iii) डिटेक्टर उपकरण:-
औद्योगिक क्षेत्रों में गैस डिटेक्टर मशीनें रिसाव की पहचान करती हैं।
(iv) स्वास्थ्य संकेत:-
अचानक सिर दर्द, सांस में तकलीफ़, चक्कर आना।
गैस रिसाव से बचाव के उपाय
(i) घरेलू स्तर पर
⇒ गैस सिलेंडर व चूल्हे की नियमित जाँच।
⇒ पाइप व रेगुलेटर समय-समय पर बदलना।
⇒ गैस इस्तेमाल करते समय वेंटिलेशन बनाए रखना।
⇒ गैस रिसाव की गंध आते ही खिड़की-दरवाजे खोलें, बिजली के उपकरण न चलाएँ।
(ii) औद्योगिक स्तर पर
⇒ गैस रिसाव डिटेक्टर और अलार्म सिस्टम लगाना।
⇒ कर्मचारियों को सुरक्षा प्रशिक्षण देना।
⇒ नियमित निरीक्षण व रखरखाव।
⇒ आपातकालीन निकासी योजना (Evacuation Plan) तैयार करना।
(iii) सरकारी व प्रशासनिक उपाय
⇒ औद्योगिक सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन।
⇒ गैस परिवहन के लिए विशेष सुरक्षा प्रावधान।
⇒ दुर्घटनाओं के बाद त्वरित राहत और पुनर्वास।
गैस रिसाव की स्थिति में क्या करें?
⇒ तुरंत सिलेंडर का रेगुलेटर बंद करें।
⇒ सभी खिड़कियाँ और दरवाजे खोलकर वेंटिलेशन बढ़ाएँ।
⇒ किसी भी प्रकार का माचिस, लाइटर या बिजली का स्विच न जलाएँ।
⇒ यदि गंध अधिक हो तो तुरंत घर/स्थान खाली करें।
⇒ निकटतम गैस आपूर्ति एजेंसी या दमकल विभाग को सूचित करें।
निष्कर्ष
गैस रिसाव एक गंभीर समस्या है जो क्षणभर में भीषण त्रासदी में बदल सकती है। इसके दुष्परिणाम केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय हानि भी पहुँचाते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
इसलिए आवश्यक है कि घरेलू, औद्योगिक और परिवहन-सभी स्तरों पर सावधानी, तकनीकी सुधार और सुरक्षा उपाय अपनाए जाएँ। प्रत्येक नागरिकों को गैस रिसाव की पहचान, बचाव और आपातकालीन कार्यवाही की जानकारी होनी चाहिए।
याद रखना चाहिए कि- “सुरक्षा में ही बचाव है।”