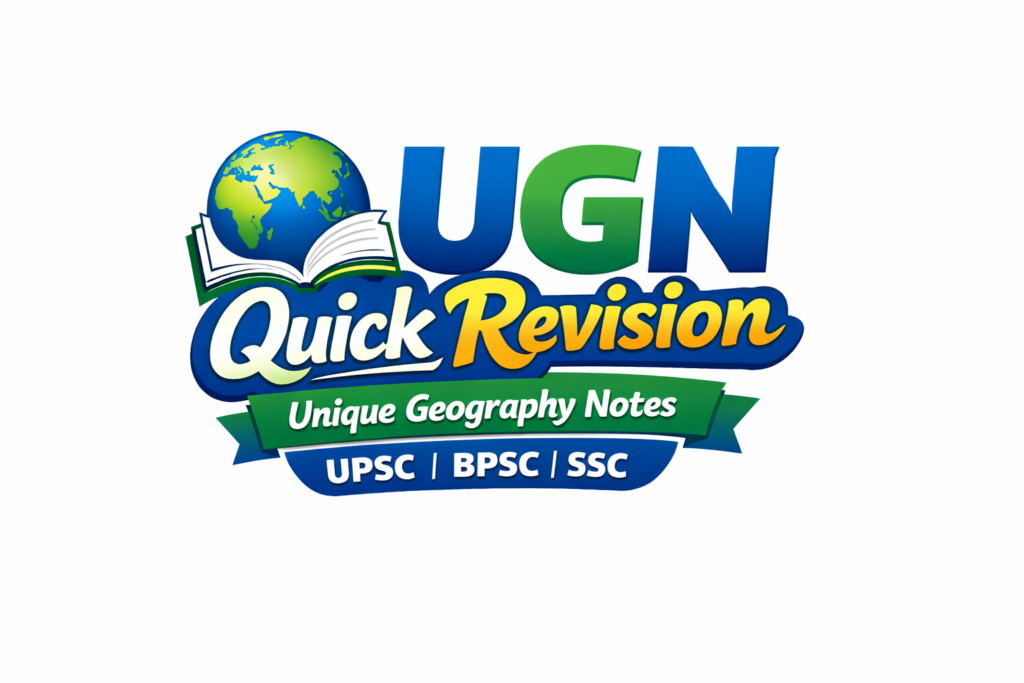41. Weather map- Difference between climate and weather (मौसम मानचित्र- जलवायु और मौसम के बीच अंतर)
Weather map- Difference between climate and weather
(मौसम मानचित्र- जलवायु और मौसम के बीच अंतर)

मौसम (Weather) की परिभाषा
मौसम किसी स्थान विशेष पर किसी निश्चित समय या अल्प अवधि (जैसे- कुछ घंटे या एक दिन) के लिए वायुमंडलीय दशाओं का सूचक होता है। यह अत्यंत परिवर्तनशील होता है, अर्थात् कुछ ही घंटों में इसमें बदलाव आ सकता है। जैसे- सुबह धूप, बादल बनना, दोपहर में वर्षा, शाम को ठंडी हवा चलना- ये सब मौसम के परिवर्तन हैं।
जलवायु (Climate) की परिभाषा
जलवायु किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का औसत है। अर्थात् यदि किसी स्थान के मौसम का 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि का औसत लिया जाए, तो वह जलवायु (Climate) कहलाता है। जैसे- राजस्थान की जलवायु शुष्क और गर्म है तथा केरल की जलवायु आर्द्र और उष्णकटिबंधीय है।
मौसम और जलवायु में अंतर
(Difference between Weather and Climate)
| क्रम | आधार | मौसम (Weather) | जलवायु (Climate) |
| 1 | समय अवधि | अल्पकालीन (कुछ घंटे या दिन) | दीर्घकालीन (30 वर्ष या अधिक) |
| 2 | क्षेत्रीय प्रभाव | छोटे क्षेत्र तक सीमित | बड़े क्षेत्र पर लागू |
| 3 | स्थायित्व | अस्थिर और परिवर्तनशील | स्थिर एवं स्थाई प्रवृत्ति |
| 4 | अध्ययन का उद्देश्य | दैनिक पूर्वानुमान | दीर्घकालीन प्रवृत्ति का विश्लेषण |
| 5 | परिवर्तन की गति | तीव्र गति से बदलता है | धीमी गति से परिवर्तन |
| 6 | उदाहरण | आज वर्षा हुई | यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है |
मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक
(i) अक्षांश (Latitude)
(ii) ऊँचाई (Altitude)
(iii) समुद्र से दूरी (Distance from Sea)
(iv) स्थलाकृति (Relief)
(v) वायु दाब और पवन प्रणाली (Pressure & Wind System)
(vi) समुद्री धाराएँ (Ocean Currents)
(vii) मानव क्रियाएँ (Human Activities)
जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पर प्रभाव
जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक समस्याओं में से एक है। यह पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण के कारण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव मौसम के पैटर्न पर देखा जा रहा है। पहले जहाँ मौसम के चक्र नियमित हुआ करते थे, वहीं अब अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी, लू, तूफान, चक्रवात और सूखे जैसी घटनाएँ बढ़ गई हैं।
इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जल संसाधनों की कमी बढ़ रही है और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने से बाढ़ की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जबकि कई क्षेत्रों में वर्षा की कमी से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। समुद्र तल में वृद्धि तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बन रही है।
इसलिए, जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। इसके समाधान के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण और वैश्विक स्तर पर सहयोग आवश्यक है, ताकि पृथ्वी की जलवायु और मौसम का संतुलन बनाए रखा जा सके।
जलवायु और मौसम का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका सीधा संबंध मानव जीवन, कृषि, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था से है। मौसम अल्पकालिक परिवर्तनों को दर्शाता है जबकि जलवायु दीर्घकालिक औसत परिस्थितियों का सूचक होती है। इन दोनों का अध्ययन छात्रों को पृथ्वी के वायुमंडलीय तंत्र, तापमान, आर्द्रता, पवन, वर्षा तथा वायुदाब जैसी घटनाओं की वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है।
शैक्षणिक दृष्टि से यह अध्ययन भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, कृषि विज्ञान, तथा आपदा प्रबंधन जैसे विषयों के लिए आधारभूत ज्ञान प्रदान करता है। इससे विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है और वे मौसम पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, तथा सतत विकास से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु तैयार होते हैं।
इसके अतिरिक्त, मौसम और जलवायु अध्ययन का उपयोग नीतिनिर्माण, जल संसाधन प्रबंधन, तथा कृषि नियोजन में भी किया जाता है। इस प्रकार, यह विषय न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान देता है बल्कि समाज के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होता है।
इस प्रकार जलवायु और मौसम का शैक्षणिक अध्ययन मानव जीवन की स्थिरता, पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक आधार प्रदान करता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
मौसम और जलवायु, दोनों पृथ्वी के वायुमंडल की प्रकृति को समझने के आधार हैं। जहाँ मौसम तात्कालिक घटनाओं का दर्पण है, वहीं जलवायु दीर्घकालीन प्रवृत्ति का चित्रण करती है। मौसम मानचित्र इन दोनों के अध्ययन को सुसंगठित, दृश्यात्मक और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम है।
यह न केवल मौसम पूर्वानुमान के लिए उपयोगी है, बल्कि कृषि, परिवहन, रक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कहा जा सकता है कि-
“मौसम मानचित्र पृथ्वी के वायुमंडलीय व्यवहार का जीवंत दस्तावेज़ है, जो मानव जीवन को सुरक्षित और संगठित बनाने में अत्यंत सहायक है।”