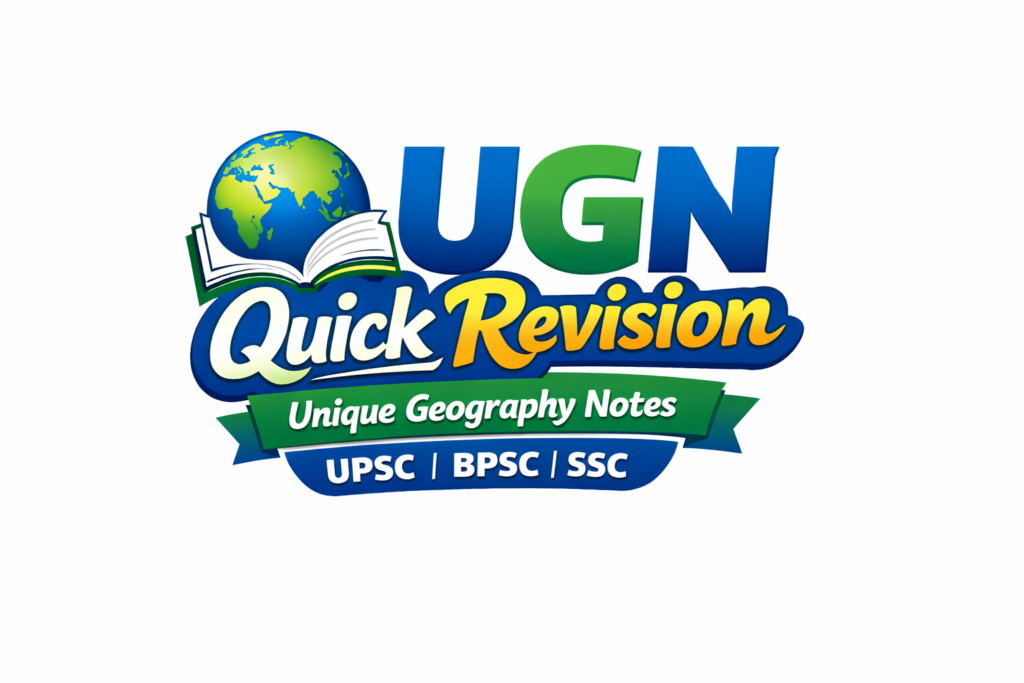29. Environmental Degradation (पर्यावरणीय क्षरण)
Environmental Degradation
(पर्यावरणीय क्षरण)

परिचय
मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही मनुष्य और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध रहा है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति से संसाधन लिए और बदले में उसे प्रभावित भी किया। आरंभिक काल में यह प्रभाव सीमित था, परंतु औद्योगिक क्रांति, तकनीकी विकास, जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण ने इस संतुलन को बिगाड़ दिया। परिणामस्वरूप आज विश्व एक गंभीर पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है जिसे “पर्यावरणीय क्षरण (Environmental Degradation)” कहा जाता है।
पर्यावरणीय क्षरण की परिभाषा
पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ है- प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता में वह गिरावट जो मानवीय या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, जिससे वायु, जल, भूमि, वन, जैव विविधता, और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्रभावित होती है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार-
“पर्यावरणीय क्षरण वह प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि जल, मृदा, वायु, वन, खनिज और जैव विविधता की गुणवत्ता और मात्रा में ह्रास होता है।”
पर्यावरणीय क्षरण के प्रमुख कारण
1. जनसंख्या वृद्धि:-
तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। भोजन, आवास और ईंधन की बढ़ती मांग ने भूमि उपयोग में असंतुलन उत्पन्न किया है। इससे वनों की कटाई, जल प्रदूषण और भूमि क्षरण जैसी समस्याएँ बढ़ी हैं।
2. औद्योगिकीकरण (Industrialization):-
औद्योगिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा में प्रदूषक गैसें (जैसे CO₂, SO₂, NO₂) उत्सर्जित होती हैं। औद्योगिक अपशिष्ट जल और ठोस कचरा नदियों और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
3. नगरीकरण (Urbanization):-
शहरीकरण की तेज प्रक्रिया ने भूमि, जल और ऊर्जा संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। कंक्रीट के जंगलों ने हरित क्षेत्रों को नष्ट किया और वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। महानगरों में ठोस अपशिष्ट और वाहनों के उत्सर्जन ने पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ दिया है।
4. वनों की कटाई (Deforestation):-
वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन खेती, चराई, खनन, और निर्माण के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है।
5. कृषि का तीव्रीकरण (Intensive Agriculture):-
रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंथेटिक पदार्थों का अत्यधिक प्रयोग मृदा और जल को विषैला बना रहा है। इससे मृदा की उर्वरता में कमी, भूजल प्रदूषण और जैव विविधता का क्षरण हुआ है।
6. खनन गतिविधियाँ (Mining Activities):-
खनन से भूमि का कटाव, जलस्रोतों का प्रदूषण और वनों का विनाश होता है। कोयला, बॉक्साइट, और लौह अयस्क जैसे खनिजों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
7. ऊर्जा उपभोग और जीवाश्म ईंधन:-
कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों को बढ़ा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या तीव्र हो गई है।
8. जल संसाधनों का दुरुपयोग:-
अतिरिक्त भूजल दोहन, प्रदूषित अपशिष्ट जल, और औद्योगिक निस्तारण के कारण जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। कई नदियाँ मृतप्राय हो चुकी हैं, जैसे- यमुना और गंगा के प्रदूषण स्तर में अत्यधिक वृद्धि।
पर्यावरणीय क्षरण के प्रकार
1. वायु प्रदूषण (Air Pollution):-
औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन धुएं और धूल कणों के कारण।
2. जल प्रदूषण (Water Pollution):-
रासायनिक अपशिष्ट, सीवेज और प्लास्टिक से।
3. मृदा क्षरण (Soil Degradation):-
रासायनिक उर्वरक, कटाव और जलभराव के कारण।
4. ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution):-
यातायात, उद्योगों और लाउडस्पीकर से उत्पन्न।
5. थर्मल और रेडियोएक्टिव प्रदूषण:-
औद्योगिक संयंत्रों और परमाणु कचरे से।
6. जैव विविधता का क्षरण (Loss of Biodiversity):-
प्राकृतिक आवासों के विनाश के कारण अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं।
पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव
(i) मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:-
वायु और जल प्रदूषण के कारण अस्थमा, कैंसर, त्वचा रोग, हृदय रोग जैसी बीमारियाँ बढ़ी हैं। WHO के अनुसार हर वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण के कारण होती है।
(ii) जलवायु परिवर्तन (Climate Change):-
ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है और चरम मौसमीय घटनाएँ (जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात) बढ़ रही हैं।
(iii) भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण:-
अधिक चराई, वनों की कटाई और जल का अत्यधिक दोहन भूमि की उत्पादकता घटाता है। यह मरुस्थलीकरण को जन्म देता है, जिससे खाद्य असुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है।
(iv) जैव विविधता में ह्रास:-
वन्यजीवों के आवास नष्ट होने से कई प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। यह पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को प्रभावित करता है।
(v) आर्थिक हानि:-
पर्यावरणीय क्षरण से कृषि उत्पादन, मत्स्य पालन, जल स्रोत, और उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है।
(vi) सामाजिक असमानता और विस्थापन:-
पर्यावरणीय क्षरण के कारण गरीब और ग्रामीण समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। जल और भूमि की कमी से “पर्यावरणीय शरणार्थी” (Environmental Refugees) की संख्या बढ़ रही है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षरण
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षरण आज मानव सभ्यता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक संसाधन दोहन के कारण पृथ्वी का पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है।
वनों की कटाई, भूमि क्षरण, जल एवं वायु प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकट विश्व स्तर पर चिंता का विषय बन चुके हैं। विकसित देशों में अत्यधिक औद्योगिक गतिविधियाँ और विकासशील देशों में अनियोजित शहरीकरण इस समस्या को और गंभीर बना रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप तापमान में वृद्धि, हिमनदों का पिघलना, समुद्र-स्तर में बढ़ोतरी तथा अनियमित वर्षा जैसी घटनाएँ मानव जीवन को सीधे प्रभावित कर रही हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-
⇒ अमेजन वर्षावन की कटाई विश्व के 20% ऑक्सीजन स्रोत को खतरे में डाल रही है।
⇒ सहारा मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका की कृषि भूमि को नष्ट कर रहा है।
⇒ आर्कटिक बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ रहा है।
⇒ भारत और चीन में वायु प्रदूषण के स्तर विश्व में सबसे ऊँचे हैं।
⇒ गंगा-यमुना जैसी नदियाँ धार्मिक महत्व के बावजूद अत्यधिक प्रदूषित हैं।
भारत में पर्यावरणीय क्षरण की स्थिति
भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और औद्योगीकरण ने पर्यावरणीय संकट को गहरा किया है।
⇒ वायु प्रदूषण: दिल्ली, कानपुर, पटना, और लखनऊ जैसे शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में हैं।
⇒ जल प्रदूषण: गंगा, यमुना, साबरमती जैसी नदियाँ औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित हैं।
⇒ वनों की कटाई: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में वनों का क्षरण तेजी से हो रहा है।
⇒ भूमि क्षरण: भारत की लगभग 30% भूमि किसी न किसी रूप में क्षतिग्रस्त है।
पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय
1. वन संरक्षण और वृक्षारोपण:-
वनों की कटाई पर नियंत्रण और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से कार्बन स्तर कम किया जा सकता है।
2. स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग:-
सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।
3. अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management):-
रीसाइक्लिंग, पुनः उपयोग और ठोस कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण आवश्यक है।
4. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण:-
उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे स्क्रबर और फिल्टर लगाना अनिवार्य होना चाहिए।
5. पर्यावरण शिक्षा:-
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य करने से जन-जागरूकता बढ़ेगी।
6. कानूनी प्रावधान:-
भारत में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 जैसे कानून लागू हैं। इनका कठोर पालन आवश्यक है।
अंतरराष्ट्रीय पहल
(i) स्टॉकहोम सम्मेलन (1972):-
स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) पर्यावरण संरक्षण हेतु पहली अंतरराष्ट्रीय पहल थी। इसमें 113 देशों ने भाग लिया और “एक पृथ्वी” के सिद्धांत को अपनाया गया। इस सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की स्थापना की, जिससे वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय नीतियों और संरक्षण प्रयासों की नींव पड़ी।
(ii) रियो अर्थ समिट (1992):-
1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो अर्थ समिट पर्यावरणीय क्षरण रोकने की एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय पहल थी। इसमें सतत विकास, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और वन प्रबंधन पर वैश्विक समझौते हुए, जिससे पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्वव्यापी सहयोग की दिशा तय हुई।
(iii) क्योटो प्रोटोकॉल (1997):-
क्योटो प्रोटोकॉल (1997) एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह विकसित देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व लगाता है ताकि वैश्विक तापवृद्धि और पर्यावरणीय क्षरण को कम किया जा सके। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा समझौते (UNFCCC) का भाग है।
(iv) पेरिस समझौता (2015):-
पर्यावरणीय क्षरण को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौता (2015) और क्योटो प्रोटोकॉल (1997) महत्वपूर्ण पहल हैं। क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने की बाध्यता डाली, जबकि पेरिस समझौते ने सभी देशों को जलवायु परिवर्तन नियंत्रण हेतु साझा जिम्मेदारी निभाने पर बल दिया।
इन सभी प्रयासों का उद्देश्य पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना और सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। हालांकि चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, परंतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है।
निष्कर्ष
इस प्रकार कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय क्षरण आज मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। यह केवल पारिस्थितिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट भी है।
यदि तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को जल, वायु और भूमि जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।अतः आवश्यक है कि मानव विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।
संरक्षण ही समाधान है– “Save Environment, Save Life.”