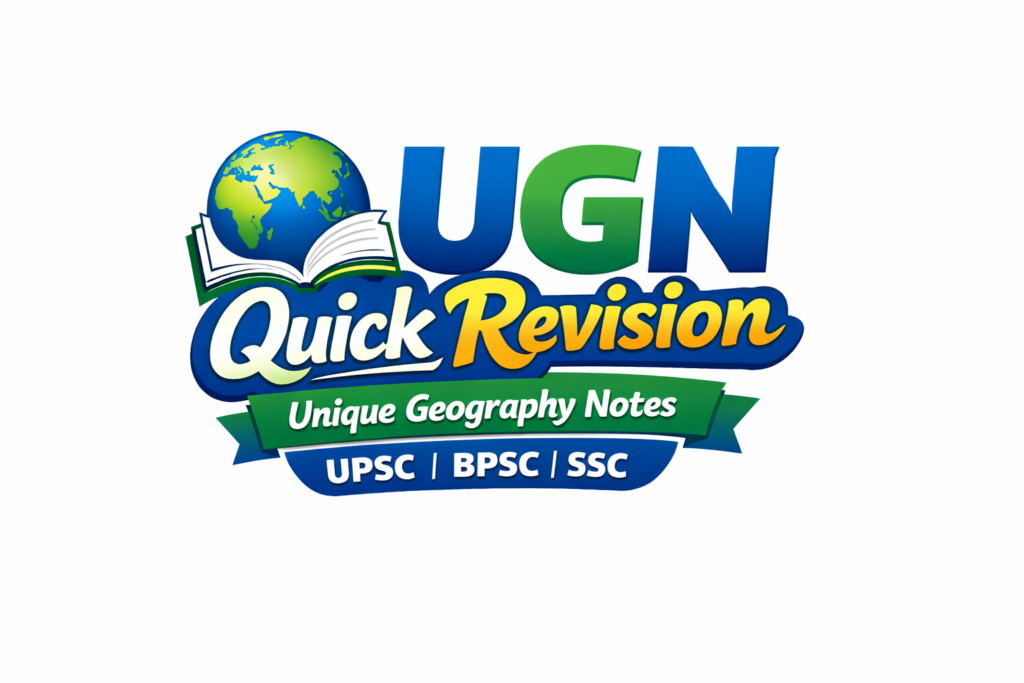26. Climatology and its Relation with Other Sciences (जलवायुविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों से इसका संबंध)
Climatology and its Relation with Other Sciences
(जलवायु विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों से इसका संबंध)
परिचय
भूगोल एक समन्वित एवं अंतर्विषयक (interdisciplinary) विज्ञान है, जो पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। इन प्राकृतिक तत्वों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल भौतिक परिदृश्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानव जीवन, कृषि, उद्योग, परिवहन, बस्तियों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है।
भौगोलिक अध्ययन में जलवायु विज्ञान (Climatology) का विशिष्ट स्थान है। यह वायुमंडल, उसके संघटन, क्रियाविधि तथा दीर्घकालिक मौसम की स्थितियों के अध्ययन से संबंधित शाखा है। जलवायु का ज्ञान केवल भूगोल तक सीमित नहीं है बल्कि मौसम विज्ञान, जीवविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक विज्ञान तक विस्तृत है।
अतः कहा जा सकता है कि जलवायु विज्ञान बहुविषयक स्वरूप वाला विज्ञान है, जो विभिन्न विषयों से अंतःक्रिया कर अपना स्वरूप विस्तारित करता है और समाज व पर्यावरण दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण बन जाता है।
परिभाषा
वायुमंडल की उन दीर्घकालिक परिस्थितियों, औसतों और प्रवृत्तियों का अध्ययन जो किसी क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु को निर्मित करती हैं, उसे जलवायु विज्ञान कहा जाता है।
W. Koppen के अनुसार– “Climatology is the science which deals with the study of average weather conditions over a long period of time.”
सरल शब्दों में कहा जाए तो मौसम की दीर्घकालिक औसत स्थिति = जलवायु और उसके वैज्ञानिक अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है।
अध्ययन क्षेत्र
⇒ वायुमंडल की संरचना व संघटन।
⇒ सौर विकिरण एवं ऊर्जा संतुलन।
⇒ तापमान, दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा के वितरण।
⇒ वैश्विक जलवायु क्षेत्र (Climate regions)।
⇒ जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ग्रीनहाउस प्रभाव।
⇒ मानव-पर्यावरण अंतःक्रिया और आपदा प्रबंधन।
महत्व
भूगोल में जलवायु का अध्ययन केवल प्राकृतिक पर्यावरण को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक क्रिया-कलापों, कृषि-पैटर्न, परिवहन मार्गों, बस्तियों के स्वरूप और सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जैसे-
⇒ मानसून एशिया में कृषि एवं जन-जीवन का निर्धारक तत्व है।
⇒ सहारा जैसे शुष्क प्रदेशों की जलवायु मानव जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती है।
⇒ शीतोष्ण कटिबंध के देश उद्योग और शहरीकरण में अग्रणी हैं, जिसका एक कारण वहाँ की अनुकूल जलवायु भी है।
इस प्रकार भूगोल में जलवायु विज्ञान का अध्ययन पृथ्वी के परिदृश्य और मानव सभ्यता की दिशा को समझने के लिए अनिवार्य है।
अन्य विज्ञानों से संबंध
जलवायु विज्ञान अन्य विज्ञानों से जुड़ा हुआ है और भूगोल के अध्ययन को समृद्ध करता है।
जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान (Meteorology)
⇒ मौसम विज्ञान वायुमंडल की अल्पकालिक घटनाओं जैसे- वर्षा, तूफान, पवन की गति, तापमान के दैनिक परिवर्तन आदि का अध्ययन करता है।
⇒ जलवायु विज्ञान इन्हीं घटनाओं के दीर्घकालिक औसत एवं प्रवृत्तियों का अध्ययन करता है।
⇒ दोनों में परस्पर गहरा संबंध है।
⇒ मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त आँकड़े ही जलवायु वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार बनते हैं।
जैसे- मानसून की भविष्यवाणी मौसम विज्ञान का कार्य है, जबकि उसका ऐतिहासिक पैटर्न और दीर्घकालिक परिवर्तन जलवायु विज्ञान का क्षेत्र है।
जलवायु विज्ञान और भौतिक भूगोल
भौतिक भूगोल (Physical Geography) पृथ्वी की सतह के प्राकृतिक घटकों-भू-आकृतियाँ, जल, मृदा, वनस्पति, जलवायु का अध्ययन करता है। इनमें से जलवायु एक प्रमुख अंग है।
(i) भू-आकृतियों पर प्रभाव- वर्षा, पवन और हिमनद जैसे जलवायुगत कारक अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण: शुष्क मरुस्थलों में पवन का कार्य और आर्द्र क्षेत्रों में वर्षा से अपक्षय।
(ii) मृदा निर्माण- मृदा की प्रकृति, उर्वरता और प्रोफ़ाइल जलवायु पर निर्भर करती है।
(iii) वनस्पति का वितरण- उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थलीय झाड़-झंखाड़, शीतोष्ण शंकुधारी वनों का स्वरूप उनकी जलवायु से जुड़ा है।
(iv) जल चक्र- भौतिक भूगोल में जल चक्र की क्रियाविधि भी तापमान और वर्षा से नियंत्रित होती है।
अतः जलवायुविज्ञान भौतिक भूगोल की रीढ़ है।
जलवायु विज्ञान और जीव-विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान
(i) जीव-जगत का वितरण- पृथ्वी पर जीव-जंतुओं और पौधों का विस्तार उनके आवास की जलवायु से जुड़ा है। जैसे- ऊँट मरुस्थल का प्रतीक है, जबकि ध्रुवीय भालू ठंडे क्षेत्रों का।
(ii) पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)- ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला और पोषण चक्र में जलवायु की प्रमुख भूमिका होती है।
(iii) जैव विविधता- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में विविधता का अधिक होना और मरुस्थलों में कम होना जलवायु का ही परिणाम है।
(iv) पर्यावरणीय संकट- जलवायु परिवर्तन से विलुप्ति का खतरा, प्रजातियों का पलायन और पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होता है।
इस प्रकार जलवायु विज्ञान जीव-विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के लिए आधार प्रदान करता है।
जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान (Oceanography)
(i) महासागरीय धाराएँ- गर्म और ठंडी धाराओं की उत्पत्ति में पवन और तापमान की भूमिका होती है।
(ii) एल-नीनो और ला-नीना- यह समुद्र-वायुमंडल की परस्पर क्रियाओं से उत्पन्न वैश्विक जलवायु घटनाएँ हैं।
(iii) समुद्री जलवायु- तटीय क्षेत्रों की आर्द्र जलवायु महासागर से प्रभावित होती है।
(iv) मछली पालन और समुद्री पारिस्थितिकी- समुद्र की सतही परतों का तापमान और ऑक्सीजन स्तर समुद्री जीवों के जीवन को नियंत्रित करते हैं।
अतः समुद्र विज्ञान और जलवायुविज्ञान दोनों परस्पर पूरक हैं।
जलवायु विज्ञान और भूविज्ञान
(i) जलवायु और चट्टानों का अपक्षय- उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, जबकि शुष्क क्षेत्रों में यांत्रिक अपक्षय।
(ii) हिमयुग और जलवायु परिवर्तन- भूवैज्ञानिक इतिहास में हिमनदों के विस्तार और संकुचन का कारण जलवायु परिवर्तन ही रहा है।
(iii) जीवाश्म और अवसादन- चट्टानों की परतें हमें पुरानी जलवायु की जानकारी देती हैं।
(iv) भूकंप और ज्वालामुखी पर प्रभाव- भूकंप और ज्वालामुखी सीधे तौर पर जलवायु नहीं बनाते, लेकिन इनके परिणाम (जैसे राख, गैस) जलवायु पर असर डालते हैं।
इस प्रकार भूविज्ञान और जलवायुविज्ञान मिलकर “पैलियोक्लाइमेटोलॉजी” (पुरा-जलवायुविज्ञान) का निर्माण करते हैं।
जलवायु विज्ञान और कृषि विज्ञान
(i) फसलों का चयन- धान, गेहूँ, मक्का, कपास जैसी फसलों का वितरण पूरी तरह से जलवायु पर निर्भर है।
(ii) कृषि कैलेंडर- बोआई, सिंचाई, कटाई आदि की समय-सीमा मानसून से निर्धारित होती है।
(iii) कृषि उत्पादकता– वर्षा की मात्रा, तापमान, आर्द्रता और धूप की अवधि उपज को नियंत्रित करती है।
(iv) कृषि संकट और आपदा- सूखा, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी जलवायु घटनाएँ कृषि को प्रभावित करती हैं।
अतः कृषि विज्ञान और जलवायु विज्ञान का संबंध अत्यंत निकट है।
जलवायु विज्ञान और जलविज्ञान (Hydrology)
जलविज्ञान पृथ्वी पर जल के वितरण, संचलन और गुणों का अध्ययन करता है। इसमें वर्षा, भूजल, सतही प्रवाह, नदियाँ, झीलें आदि सम्मिलित हैं।
(i) वर्षा और नदी प्रवाह- किसी नदी के जलस्रोत का आकार और प्रवाह सीधे वर्षा की मात्रा और वितरण पर निर्भर करता है।
(ii) बाढ़ और सूखा- ये दोनों जलवायुगत घटनाएँ जलविज्ञान के अध्ययन का मूल विषय हैं।
(iii) भूजल पुनर्भरण- आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर में बहुत अंतर पाया जाता है।
(iv) जल चक्र (Hydrological Cycle)- वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा और प्रवाह ये सभी प्रक्रियाएँ जलवायु के नियंत्रण में होती हैं।
इस प्रकार जलविज्ञान और जलवायुविज्ञान का संबंध अत्यंत गहरा और पारस्परिक है।
जलवायु विज्ञान और मानव भूगोल/अर्थशास्त्र
जलवायु केवल प्राकृतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह मानव समाज और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालती है।
(i) बस्तियों का वितरण- मानव बस्तियाँ प्रायः अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं।
(ii) कृषि और अर्थव्यवस्था- मानसून-आधारित कृषि अर्थव्यवस्था भारत जैसे देशों में जलवायु पर निर्भर है।
(iii) उद्योग और ऊर्जा- हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सीधे जलवायुगत परिस्थितियों पर आधारित हैं।
(iv) परिवहन और व्यापार- समुद्री मार्गों, हवाई मार्गों और स्थल परिवहन की सुगमता जलवायु से प्रभावित होती है।
(v) स्वास्थ्य और जीवनशैली- रोगों का प्रसार, पोशाक, भोजन और आवास की शैली जलवायु के अनुसार ढलती है।
इस प्रकार जलवायुविज्ञान मानव भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों के अध्ययन में केंद्रीय स्थान रखता है।
जलवायु विज्ञान और गणितीय/सांख्यिकीय विज्ञान
आधुनिक युग में जलवायुविज्ञान के अध्ययन में गणित और सांख्यिकी का विशेष योगदान है।
(i) डेटा विश्लेषण- तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब आदि के आँकड़ों को सांख्यिकीय तकनीकों से विश्लेषित किया जाता है।
(ii) मॉडल निर्माण- भविष्यवाणी हेतु गणितीय समीकरणों और मॉडलों का उपयोग किया जाता है।
(iii) संभाव्यता अध्ययन- बाढ़, सूखा या तूफ़ान जैसी घटनाओं की संभावना सांख्यिकी के आधार पर आंकी जाती है।
(iv) स्थानिक आँकड़ा विश्लेषण (Spatial Statistics)- GIS और Remote Sensing से प्राप्त आँकड़ों का गणितीय प्रसंस्करण।
इससे जलवायुविज्ञान अधिक वैज्ञानिक और सटीक बन पाया है।
जलवायु विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान (Remote Sensing एवं GIS)
आधुनिक तकनीक ने जलवायु विज्ञान के अध्ययन को नई दिशा दी है।
(i) Remote Sensing (दूरसंवेदी तकनीक)- उपग्रहों से प्राप्त आँकड़े वायुमंडल और सतह की स्थितियों को मापने में मदद करते हैं।
(ii) GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली)- जलवायु से संबंधित स्थानिक आँकड़ों को संग्रहित, विश्लेषित और मानचित्रित करने में GIS का उपयोग होता है।
(iii) Climate Models- सुपर कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से भविष्य की जलवायु परिवर्तन प्रवृत्तियों का आकलन किया जाता है।
(iv) Artificial Intelligence और Machine Learning- अब जलवायु की भविष्यवाणी और जोखिम आकलन में इन तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है।
जलवायु विज्ञान का बहुविषयक स्वरूप
उपरोक्त सभी संबंधों से स्पष्ट है कि जलवायुविज्ञान एक बहुविषयक (Interdisciplinary) विज्ञान है।
⇒ यह भौतिक विज्ञान (भौतिकी, गणित, रसायन) पर आधारित है।
⇒ यह जीव विज्ञान और पारिस्थितिकी से जुड़ा है।
⇒ यह सामाजिक और आर्थिक विज्ञान से भी संबंधित है।
⇒ यह तकनीकी विज्ञान (कंप्यूटर, GIS, Remote Sensing) का उपयोग करता है।
इस प्रकार जलवायुविज्ञान केवल भूगोल की शाखा नहीं है बल्कि अनेक विज्ञानों का संगम है।
समकालीन चुनौतियाँ और जलवायु विज्ञान
21वीं शताब्दी में जलवायु से संबंधित समस्याएँ वैश्विक स्तर पर मानव सभ्यता के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हैं।
(i) जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
⇒ औद्योगिक क्रांति के बाद से ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, CH₄, N₂O) का उत्सर्जन बढ़ा।
⇒ इसके कारण औसत वैश्विक तापमान निरंतर बढ़ रहा है।
⇒ ध्रुवीय हिमनद पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है।
(ii) वैश्विक तापन (Global Warming)
⇒ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) की रिपोर्टों के अनुसार 2100 तक वैश्विक तापमान 1.5°C से 3°C तक बढ़ सकता है।
⇒ इसका असर कृषि, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पारिस्थितिकी पर पड़ेगा।
(iii) चरम जलवायु घटनाएँ (Extreme Climate Events)
⇒ चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव और कोल्ड वेव जैसी घटनाएँ बार-बार घट रही हैं।
⇒ भारत में 2015 की चेन्नई बाढ़, 2020 का अम्फान चक्रवात और 2023 की हीट वेव इसके उदाहरण हैं।
(iv) आपदा प्रबंधन (Disaster Management)
⇒ जलवायुविज्ञान आज आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।
⇒ मौसम पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग से जान-माल की क्षति कम करने में मदद मिलती है।
भौगोलिक अध्ययनों में जलवायु विज्ञान का महत्व
भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंध को समझना है। इस संदर्भ में जलवायु विज्ञान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
(i) मानव-पर्यावरण संबंध- भूगोल में मनुष्य और पर्यावरण की अंतःक्रिया को जलवायु के आधार पर समझा जाता है।
(ii) क्षेत्रीय अध्ययन- किसी भी क्षेत्र की विशेषताओं (जैसे कृषि, बस्तियाँ, जीवनशैली) के निर्धारण में जलवायु प्रमुख कारक है।
(iii) नक्शा-निर्माण और वर्गीकरण- Koppen और Thornthwaite जैसे जलवायु वर्गीकरण भूगोल को वैज्ञानिक आधार देते हैं।
(iv) अनुसंधान और नीति-निर्माण- जलवायुविज्ञान जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और आपदा प्रबंधन संबंधी नीतियों के लिए आवश्यक आँकड़े और विश्लेषण उपलब्ध कराता है।
निष्कर्ष
जलवायु विज्ञान भूगोल की एक केंद्रीय शाखा है, जो पृथ्वी के वायुमंडलीय घटनाओं और उनके दीर्घ कालिक स्वरूप का अध्ययन करती है। यह केवल मौसम के औसत की गणना भर नहीं है, बल्कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, जैविक और तकनीकी सभी पहलुओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
⇒ मौसम विज्ञान, भूगोल, जीवविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, समुद्र विज्ञान, कृषि विज्ञान, जलविज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और कंप्यूटर विज्ञान- इन सभी से इसका गहरा संबंध है।
⇒ समकालीन युग में जब जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है, तब जलवायुविज्ञान का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।
⇒ यह न केवल हमें भौगोलिक परिदृश्य और मानव समाज की समझ प्रदान करता है, बल्कि भविष्य की नीतियों और विकास की दिशा भी निर्धारित करता है।
अतः जलवायु विज्ञान एक ऐसा अंतर्विषयक विज्ञान है जो भूगोल को बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है और मानवता को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करता है।