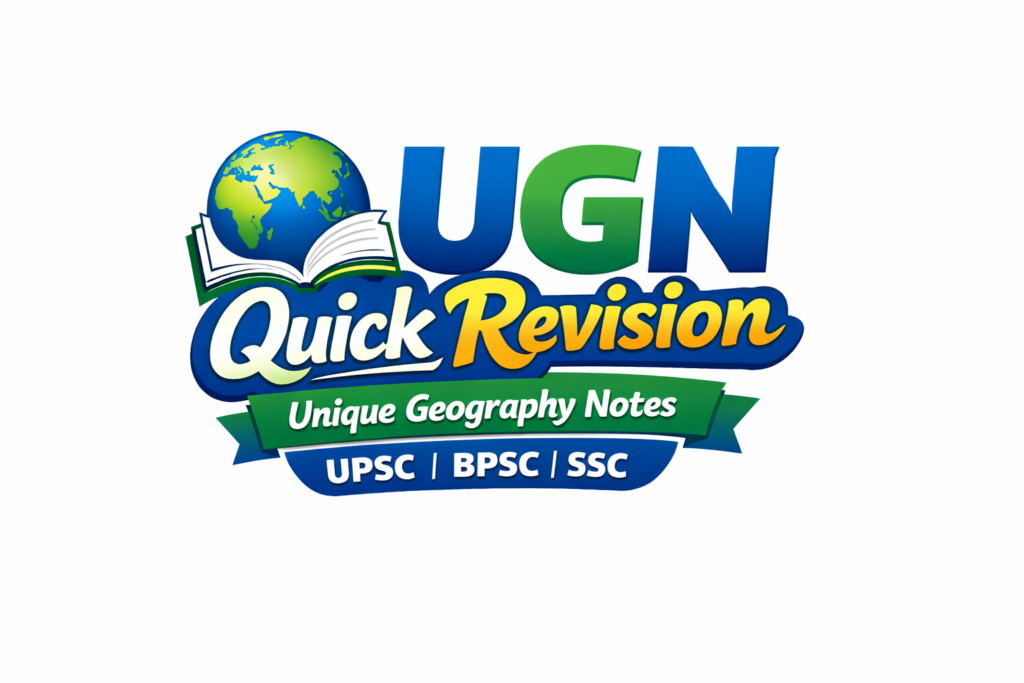28. Environmental Geography: Meaning and Concept (पर्यावरणीय भूगोल : अर्थ और अवधारणा)
Environmental Geography: Meaning and Concept
(पर्यावरणीय भूगोल : अर्थ और अवधारणा)
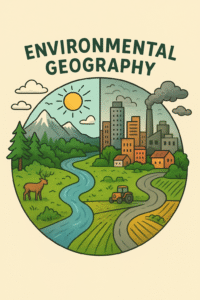
मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भूगोल की मुख्य विषयवस्तु रहा है। भूगोल विषय का सबसे प्रमुख लक्ष्य यह समझना है कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर प्राकृतिक एवं मानव निर्मित प्रक्रियाएँ एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं। इस दृष्टि से पर्यावरणीय भूगोल (Environmental Geography) भूगोल का एक ऐसा शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्संबंधों, पारिस्थितिक असंतुलनों, पर्यावरणीय संकटों और उनके समाधान की खोज करता है।
वास्तविक में पर्यावरणीय भूगोल का विकास 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तब हुआ जब औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या विस्फोट और संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया। यह शाखा मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच एक सेतु का कार्य करती है।
पर्यावरण (Environment) का अर्थ
“पर्यावरण” शब्द संस्कृत के “परि + आवरण” से बना है जिसका अर्थ है – चारों ओर से घेरने वाला आवरण। अर्थात् वह सब कुछ जो किसी जीव या मानव को चारों ओर से घेरता है और उसके जीवन को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है।
अंग्रेजी में, Environment का अर्थ है- “The surroundings or conditions in which a person, animal, or plant lives and operates.”
पर्यावरण के प्रकार
पर्यावरण मुख्यतः दो प्रकार का होता है-
1. प्राकृतिक पर्यावरण (Natural Environment):-
इसमें वायु, जल, मृदा, वनस्पति, जीव-जंतु, पर्वत, नदियाँ आदि तत्व शामिल होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है।
2. मानव निर्मित पर्यावरण (Human-made Environment):-
यह मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बनाया गया है, जैसे भवन, सड़कें, उद्योग, परिवहन साधन आदि।
इन दोनों प्रकार के पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि असंतुलन से प्रदूषण और पारिस्थितिक संकट उत्पन्न होते हैं।
पर्यावरणीय भूगोल का अर्थ
(Meaning of Environmental Geography)
पर्यावरणीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो प्राकृतिक पर्यावरण और मानव क्रियाकलापों के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यह मानव के पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरणीय संकट, प्रदूषण, संसाधनों का संरक्षण, और सतत विकास जैसे मुद्दों पर केन्द्रित है।
सरल शब्दों में-
पर्यावरणीय भूगोल वह विज्ञान है जो यह समझने का प्रयास करता है कि “मानव अपने पर्यावरण को कैसे परिवर्तित करता है और पर्यावरण इन परिवर्तनों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।”
पर्यावरणीय भूगोल की परिभाषाएँ (Definitions)
G. T. Trewartha (1968) के अनुसार – “Environmental Geography is the study of the mutual relationship between man and his physical environment.”
Strahler (1971) के अनुसार – “It is the study of the environment as the home of man and the interrelationship between physical and cultural elements.”
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार – “पर्यावरणीय भूगोल पृथ्वी के भौतिक, जैविक, सामाजिक और आर्थिक घटकों के पारस्परिक अंतःक्रियाओं का समन्वित अध्ययन है।”
पर्यावरणीय भूगोल का विकास
(Development of Environmental Geography)
पर्यावरणीय भूगोल का विकास चार मुख्य चरणों में हुआ-
1. प्रारंभिक चरण (Pre-scientific Phase):-
प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने अपने ग्रंथ “On Airs, Waters, and Places” में पर्यावरण के मानव जीवन पर प्रभाव का उल्लेख किया। भारत में भी “पंचतत्व” और “भूमि-जल-वायु-सूर्य” जैसे सिद्धांत पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित थे।
2. पर्यावरणीय नियतिवाद (Environmental Determinism)
19वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोलवेत्ताओं ने यह माना कि मानव जीवन पूरी तरह प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे- गर्म जलवायु वाले लोग आलसी और ठंडे प्रदेशों के लोग परिश्रमी होते हैं।
मुख्य समर्थक- Ratzel, Semple, Huntington।
3. संभाव्यवाद (Possibilism)
20वीं शताब्दी में Lucien Febvre और Vidal de la Blache ने कहा कि पर्यावरण सीमाएँ तो निर्धारित करता है, परंतु मानव अपनी बुद्धि से उन्हें पार कर सकता है।
4. पर्यावरणीय पुनर्जागरण (Neo-environmentalism)
1960 के बाद वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, और पारिस्थितिक संकटों के कारण “Environmental Geography” एक स्वतंत्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ।
पर्यावरणीय भूगोल की प्रमुख अवधारणाएँ
(Major Concepts in Environmental Geography)
पर्यावरणीय भूगोल की प्रमुख अवधारणाएँ निम्नलिखित है-
(i) पर्यावरणीय संतुलन (Environmental Balance):-
यह स्थिति तब होती है जब प्राकृतिक घटक जैसे भूमि, जल, वायु, और जीव-जंतु अपने प्राकृतिक रूप में संतुलित रहते हैं।
(ii) पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem):-
जैविक और अजैविक घटकों का एक ऐसा तंत्र जो ऊर्जा और पदार्थ के आदान-प्रदान से संचालित होता है।
(iii) मानव-पर्यावरण पारस्परिकता
(Man-Environment Interaction):-
यह अध्ययन करता है कि मानव गतिविधियाँ (जैसे- कृषि, उद्योग, नगरीकरण) पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं और इसके परिणामस्वरूप कौन से संकट उत्पन्न होते हैं।
(iv) सतत विकास (Sustainable Development):-
वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों के संसाधनों से समझौता न करना।
(v) पर्यावरणीय संकट (Environmental Crisis):-
जैसे- जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, मरुस्थलीकरण, ओजोन परत में छिद्र, जैव विविधता का ह्रास आदि।
पर्यावरणीय भूगोल का अध्ययन क्षेत्र
(Scope of Environmental Geography)
पर्यावरणीय भूगोल का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं-
(i) प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उपयोग
(ii) भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण परिवर्तन (Land Use/Land Cover Change)
(iii) जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव
(iv) प्रदूषण अध्ययन- वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि
(v) जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण
(vi) मानव बस्तियों और नगरीकरण के पर्यावरणीय प्रभाव
(vii) आपदा प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन (Disaster Management & Risk Assessment)
(viii) पर्यावरणीय नीति और योजना निर्माण (Environmental Planning & Policy)
पर्यावरणीय भूगोल और अन्य शाखाओं का संबंध
(i) भौतिक भूगोल- पर्यावरणीय तत्वों का आधार (भूमि, जल, वायु)
(ii) मानव भूगोल- मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव
(iii) आर्थिक भूगोल- संसाधनों के दोहन और प्रबंधन से जुड़ा
(iv) पारिस्थितिकी- जैविक और अजैविक तंत्रों का अध्ययन
(v) भू-स्थानिक विज्ञान (GIS/RS)- पर्यावरणीय डेटा का विश्लेषण
आधुनिक युग में पर्यावरणीय भूगोल की उपयोगिता
आधुनिक युग में पर्यावरणीय भूगोल की उपयोगिता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता करता है। तीव्र औद्योगीकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है।
पर्यावरणीय भूगोल भूमि, जल, वायु, जैव विविधता तथा मानव क्रियाओं के प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करता है। यह सतत विकास की दिशा में नीतियों के निर्माण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और आपदा प्रबंधन में भी सहायक है। इस प्रकार, आधुनिक युग में पर्यावरणीय भूगोल मानव और प्रकृति के संतुलन हेतु अपरिहार्य है।
निष्कर्ष:-
निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि यह मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान तथा सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना है।
यह भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से पर्यावरणीय परिवर्तन, प्रदूषण, भूमि उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि का विश्लेषण करता है। पर्यावरणीय भूगोल मानव क्रियाओं के प्रभावों को समझकर प्रकृति के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, यह आधुनिक भूगोल का एक आवश्यक और व्यावहारिक अंग है।