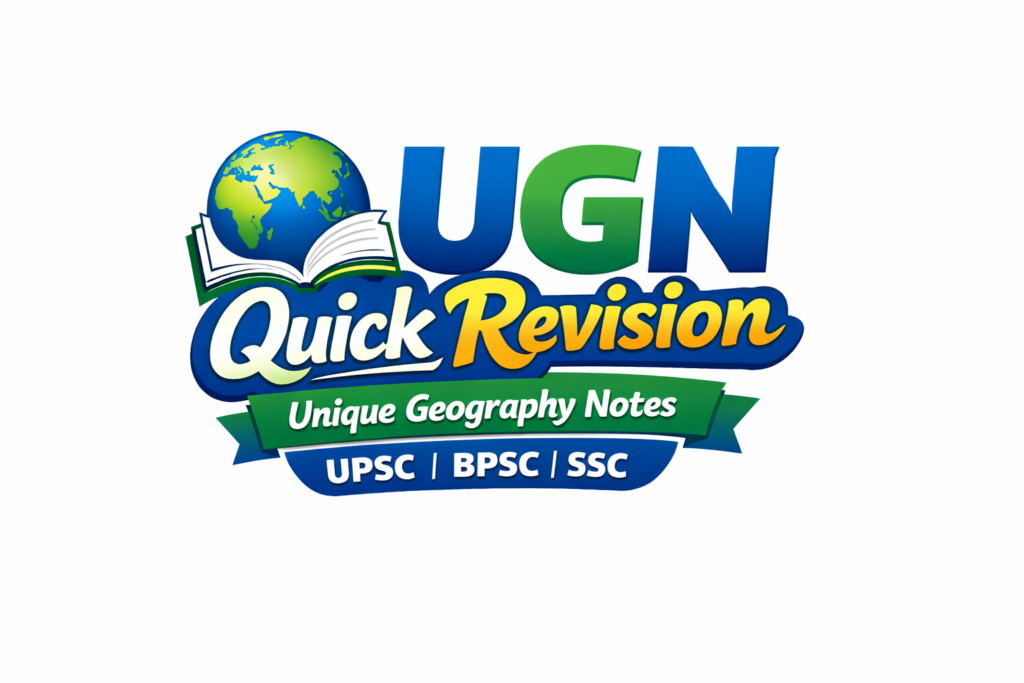31. Environmental management and policies (पर्यावरण प्रबंधन और नीतियाँ)
Environmental management and policies
(पर्यावरण प्रबंधन और नीतियाँ)

परिचय
वर्तमान समय में पर्यावरणीय असंतुलन विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन ने पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरणीय नीतियाँ वह प्रमुख उपकरण हैं, जिनके माध्यम से हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं।
पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा
पर्यावरण प्रबंधन (Environmental Management) का अर्थ है- मानव और पर्यावरण के बीच संतुलित संबंध बनाए रखना, ताकि विकास की प्रक्रिया पर्यावरण को नष्ट न करे, बल्कि उसे सुरक्षित रखते हुए सतत् विकास सुनिश्चित करे। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें नीति-निर्माण, संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा उपयोग, तथा सामाजिक सहभागिता जैसे तत्व शामिल हैं।
पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य
पर्यावरण प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य है-
(i) प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग करना।
(ii) प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करना।
(iii) जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना।
(iv) पर्यावरण शिक्षा और जनजागरूकता का प्रचार-प्रसार करना।
(v) सतत् विकास के सिद्धांतों का पालन करना।
(vi) पर्यावरणीय आपदाओं से निपटने की क्षमता विकसित करना।
पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख घटक
पर्यावरण प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव और प्राकृतिक संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है ताकि विकास और पर्यावरण दोनों का संरक्षण हो सके। इसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं-
1. नीतिगत घटक (Policy Component):-
यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन से जुड़ा होता है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आदि।
2. संगठनात्मक घटक (Institutional Component):-
विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, UNEP, WWF आदि पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
3. तकनीकी घटक (Technical Component):-
पर्यावरणीय निगरानी, प्रदूषण नियंत्रण तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन, तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) इसके अंतर्गत आते हैं।
4. सामाजिक एवं शैक्षणिक घटक (Social & Educational Component):-
जन-जागरूकता, पर्यावरण शिक्षा, और स्थानीय समुदायों की सहभागिता से पर्यावरणीय नीतियों को प्रभावी बनाया जाता है।
5. आर्थिक घटक (Economic Component):-
हरित अर्थव्यवस्था, सतत विकास, और प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक मूल्यांकन पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करते हैं।
इन सभी घटकों का समन्वय ही प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन की आधारशिला बनाता है, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित होता है।
पर्यावरण प्रबंधन के साधन
पर्यावरण प्रबंधन के साधन वे उपाय हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण की गुणवत्ता को संरक्षित, सुधारित और संतुलित किया जाता है। इनका उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख साधनों को चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है-
(1) नीतिगत साधन,
(2) विधिक साधन,
(3) आर्थिक साधन, और
(4) शैक्षणिक एवं तकनीकी साधन।
(1) नीतिगत साधन:–
सरकार द्वारा बनाई गई पर्यावरण नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, वन नीति आदि।
(2) विधिक साधन:-
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981 आदि कानूनों के माध्यम से पर्यावरणीय अपराधों पर नियंत्रण।
(3) आर्थिक साधन:-
प्रदूषण कर, हरित कर, अनुदान, प्रोत्साहन, और पर्यावरणीय बीमा जैसी आर्थिक व्यवस्थाएँ, जो उद्योगों को स्वच्छ तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित करती हैं।
(4) शैक्षणिक एवं तकनीकी साधन:-
पर्यावरण शिक्षा, जनजागरूकता, और आधुनिक तकनीकी उपाय जैसे पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।
भारत में पर्यावरण प्रबंधन का विकास
भारत में पर्यावरण संरक्षण की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में प्रकृति के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना विद्यमान रही है। स्वतंत्रता के पश्चात औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ीं, जिससे सरकार ने संगठित पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए।
अर्थात भारत में पर्यावरण प्रबंधन का विकास एक दीर्घकालीन प्रक्रिया रही है, जो पारंपरिक जीवनशैली से आधुनिक नीतियों तक फैली हुई है। प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा माना जाता था। वन, जल, भूमि और पशुओं के प्रति आदर की भावना वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ीं, जिससे वैज्ञानिक और नीतिगत स्तर पर पर्यावरण प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई।
1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। 1976 में संविधान में अनुच्छेद 48A और 51A(g) जोड़े गए, जिनमें राज्य और नागरिकों के पर्यावरण संरक्षण के दायित्व का उल्लेख है।
1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया, जिसने देश में पर्यावरण नीति का कानूनी आधार प्रदान किया। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति (1988), जैव विविधता अधिनियम (2002) तथा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (2008) जैसी पहलें की गईं।
आज भारत सतत विकास और हरित तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत बना रहा है। सरकारी योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, और जल जीवन मिशन ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
भारत की प्रमुख पर्यावरण नीतियाँ
1. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति (National Environment Policy, 2006):-
⇒ सतत् विकास, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन को एकीकृत करने का प्रयास।
⇒ विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) को अनिवार्य किया गया।
⇒ स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर बल।
2. राष्ट्रीय वन नीति (National Forest Policy, 1988):-
⇒ देश के कम से कम 33% भूभाग पर वनावरण बनाए रखने का लक्ष्य।
⇒ सामाजिक वनीकरण एवं संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम।
3. राष्ट्रीय जल नीति (National Water Policy, 2012):-
⇒ जल का समान वितरण, पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग को बढ़ावा।
⇒ जल संरक्षण हेतु सामुदायिक भागीदारी।
4. राष्ट्रीय जैव विविधता नीति (National Biodiversity Policy, 2002):-
⇒ पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता की रक्षा।
⇒ पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा और जैव संसाधनों का सतत् उपयोग।
5. राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC, 2008):-
⇒ आठ मिशनों पर आधारित नीति, जैसे सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, जल मिशन आदि।
⇒ कार्बन उत्सर्जन घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग पर बल।
भारत में प्रमुख पर्यावरणीय कानून
1. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
⇒ जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना।
2. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
⇒ वायु गुणवत्ता मानकों का निर्धारण एवं प्रदूषकों के उत्सर्जन पर नियंत्रण।
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
⇒ यह अधिनियम सभी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए “छत्र कानून” के रूप में कार्य करता है।
⇒ सरकार को पर्यावरणीय मानक निर्धारित करने और दंड लगाने की शक्ति देता है।
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
⇒ वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा।
⇒ संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना।
5. वन संरक्षण अधिनियम, 1980
⇒ वनों की कटाई पर नियंत्रण और वन भूमि के उपयोग में बदलाव पर रोक।
6. जैव विविधता अधिनियम, 2002
⇒ स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान की रक्षा और जैव संसाधनों के उपयोग का नियमन।
अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीतियाँ और भारत की भूमिका
भारत वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों में सक्रिय भागीदार रहा है।
1. स्टॉकहोम सम्मेलन (1972):- भारत ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की।
2. रियो अर्थ समिट (1992):- सतत् विकास की अवधारणा को भारत ने नीति में शामिल किया।
3. क्योटो प्रोटोकॉल (1997):- भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लिए स्वैच्छिक पहल की।
4. पेरिस समझौता (2015):- भारत ने 2030 तक 40% बिजली उत्पादन को नवीकरणीय ऊर्जा से करने का संकल्प लिया।
पर्यावरणीय संस्थान और संगठन
(i) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
(iii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)
(iv) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)- पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए।
(v) TERI, NEERI, WWF-India, और CSE जैसे गैर-सरकारी संस्थान भी सक्रिय हैं।
पर्यावरण प्रबंधन की चुनौतियाँ
⇒ तीव्र औद्योगिकीकरण और नगरीकरण।
⇒ जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों का अति-दोहन।
⇒ पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता का अभाव।
⇒ नीति क्रियान्वयन में प्रशासनिक ढिलाई।
⇒ तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की कमी।
नवीन पहलें
⇒ स्वच्छ भारत अभियान
⇒ नमामि गंगे परियोजना
⇒ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
⇒ अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन
⇒ हरित भारत मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
जनसहभागिता और पर्यावरण प्रबंधन
पर्यावरणीय नीतियों की सफलता नागरिकों की भागीदारी पर निर्भर करती है।गाँवों में जल, वन, भूमि प्रबंधन समितियाँ; शहरों में कचरा प्रबंधन, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आंदोलन। ये सब जनसहभागिता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
निष्कर्ष
पर्यावरण प्रबंधन और नीतियाँ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि यह मानव अस्तित्व और जीवन गुणवत्ता की रक्षा का आधार हैं। यदि विकास पर्यावरण के विरुद्ध होगा, तो वह अंततः मानवता के विरुद्ध होगा। अतः आवश्यक है कि हम “विकास और पर्यावरण संरक्षण” के बीच सामंजस्य बनाकर सतत् विकास की दिशा में आगे बढ़ें।
पर्यावरण संरक्षण केवल कानूनों या योजनाओं से नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और सामूहिक प्रयास से संभव है। तभी पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध रह सकेगी।