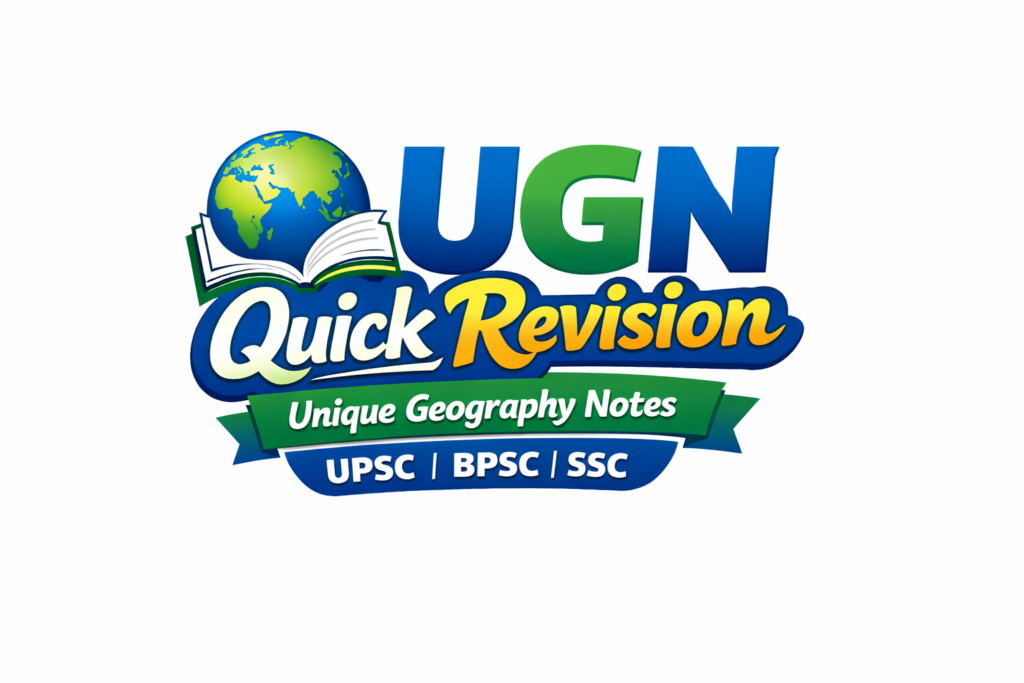Chapter 10 Atmospheric Circulation and Weather Systems (वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ)
Chapter 10 Atmospheric Circulation and Weather Systems
(वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ)
(भाग – 1 : भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत)
बिहार बोर्ड तथा NCERT कक्षा 11वीं के भूगोल का सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर
1. बहुवैकल्पिक प्रश्न एवं उनके उत्तर
(i) यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो घरातल से 1 किमी की ऊँचाई पर वायुदाब कितना होगा?
(क) 700 मिलीबार
(ख) 900 मिलीबार
(ग) 1100 मिलीबार
(घ) 1300 मिलीबार
उत्तर- (ख) 900 मिलीबार
व्याख्या:
सामान्यतः धरातल से ऊँचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। औसत रूप से हर 1 किलोमीटर ऊँचाई पर वायुदाब लगभग 100 मिलीबार कम हो जाता है। यदि धरातल पर वायुदाब = 1000 मिलीबार है, तो 1 किमी ऊँचाई पर वायुदाब लगभग = 1000 – 100 = 900 मिलीबार होगा।
(ii) अंतर ऊष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है?
(क) भूमध्य रेखा के निकट
(ख) कर्क रेखा के निकट
(ग) मकर रेखा के निकट
(घ) आर्कटिक वृत्त के निकट
उत्तर- (क) भूमध्य रेखा के निकट
व्याख्या:
अंतर ऊष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (Inter Tropical Convergence Zone – ITCZ) वह क्षेत्र है जहाँ उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें (Trade Winds) आपस में मिलती हैं।
यह क्षेत्र सामान्यतः भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है, हालांकि यह सूर्य के वार्षिक गमन के अनुसार कर्क और मकर रेखा के बीच थोड़ा-बहुत उत्तर-दक्षिण की ओर खिसकता रहता है।
(iii) उत्तरी गोलार्द्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी?
(क) घड़ी की सुईयों के चलने की दिशा के अनुरूप
(ख) घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत
(ग) समदाब रेखाओं के समकोण पर
(घ) समदाब रेखाओं के सामानंतर
उत्तर- (ख) घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत
व्याख्या:
उत्तरी गोलार्द्ध में निम्न वायुदाब (Low Pressure) क्षेत्र के चारों तरफ पवनें कोरिऑलिस बल के प्रभाव से घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमती हैं। इसे साइक्लोनिक परिसंचरण भी कहा जाता है—यह भीतर की ओर और वामावर्त (Anticlockwise) दिशा में होता है।
(iv) वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन-सा है?
(क) विषुवतीय वन
(ख) साइबेरिया का मैदानी भाग
(ग) हिमालय पर्वत
(घ) दक्कन पठार न पठार
उत्तर- (ख) साइबेरिया का मैदानी भाग
व्याख्या :
वायुराशियों (Air Masses) के निर्माण के लिए ऐसे क्षेत्र चाहिए होते हैं जहाँ-
विशाल भूभाग या महासागर हों,
सतह समान प्रकृति की हो,
मौसम लम्बे समय तक स्थिर रहे (High Pressure / Anticyclonic conditions)।
साइबेरिया का मैदानी भाग एक विशाल, ठंडा, स्थिर उच्च दाब वाला क्षेत्र है, जहाँ शुष्क एवं ठंडी महाद्वीपीय वायु राशियाँ आसानी से बनती हैं।
बाकी विकल्प वायुराशियों के उद्गम क्षेत्र नहीं माने जाते-
विषुवतीय वन- यहाँ तीव्र संवहन होता है, वायुराशि स्थिर नहीं रहती।
हिमालय पर्वत- पर्वतीय क्षेत्र वायुराशियों के उद्गम के लिए उपयुक्त नहीं।
दक्कन पठार- अपेक्षाकृत छोटा व विविध तापमान वाला क्षेत्र, स्थिर वायुराशियाँ नहीं बनतीं।
अतः सही विकल्प- (ख)
(v) निम्नलिखित में कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है?
(क) दाब प्रवलता
(ख) अभिकेंद्रीय लक्षण
(ग) कोरियोलीसि
(घ) भू-घर्षण
उत्तर- (ग) कोरियोलीसि
(क) 65 मी०
(ख) 165 मी०
(ग) 500 मी०
(घ) 1000 मी०
उत्तर- (ख) 165 मी०
व्याख्या:
वायुमंडल में सामान्य lapse rate के अनुसार हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान लगभग 1°C घट जाता है। इसे सामान्य अवरोही ताप प्रवणता (Normal Lapse Rate) कहा जाता है, जो लगभग 6.5°C प्रति 1000 मीटर के बराबर होती है।
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए
(i) वायुदाब मापने की इकाई क्या है? मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है?
उत्तर- वायुदाब की माप की इकाई मिलीबार (mb) या हेक्टोपास्कल (hPa) है। मौसम मानचित्र बनाते समय विभिन्न स्थानों की ऊँचाई अलग-अलग होती है, इसलिए तुलना को समान आधार पर लाने हेतु वायुदाब को समुद्र तल के दबाव तक घटाकर दिखाया जाता है।
(ii) जब दाब प्रवणता बल उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हो अर्थात् उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत् वृत की ओर हो तो उत्तरी गोलार्द्ध में उष्णकटिबंध में पवनें उत्तरी-पूर्वी क्यों होती हैं?
उत्तर- उत्तरी गोलार्द्ध में दाब प्रवणता बल उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत् रेखा की ओर पवनों को दक्षिण की ओर धकेलता है, लेकिन कोरियोलिस बल उन्हें दाईं ओर मोड़ देता है। परिणामस्वरूप पवनों की दिशा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और वे उत्तर-पूर्वी व्यापारिक पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं।
(iii) भूविक्षेपी पवनें (Geotrophic winds) क्या हैं?
उत्तर- भूविक्षेपी पवनें वे हवाएँ हैं जो वायुदाब-ढाल बल और कोरिओलिस बल के संतुलन में उच्च दाब से निम्न दाब की दिशा में समोच्च दबाव रेखाओं (Isobars) के समानांतर बहती हैं। ये ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती हैं और इन पर घर्षण का प्रभाव बहुत कम होता है।
(iv) समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करें।
उत्तर- स्थल समीर और समुद्र समीर (Land Breeze and Sea Breeze)
➤ दिन के समय समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र, समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं जिससे स्थल पर LP का और समुद्र पर HP का निर्माण हो जाता है जिससे हवा समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होने लगती है, इसे सागरीय या समुद्री समीर कहते हैं।
➤ इसके विपरीत रात के समय पार्थिव विकिरण के कारण स्थलीय भाग सागरीय भाग की तुलना में शीघ्रता से ठंडी हो जाती है जिससे स्थल पर HP एवं समुद्र पर LP का निर्माण होता है, जिसके कारण हवा स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं।


(v) पवनों की दिशा एवं गति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
उत्तर- पवनों की दिशा एवं गति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं-
➤ तापीय एवं दाब भिन्नता
➤ पृथ्वी का घूर्णन (कोरिओलिस बल)
➤ घर्षण बल (स्थल एवं जल सतह)
➤ भू-आकृति (पहाड़, घाटियाँ)
➤ ऋतु एवं मौसम संबंधी परिस्थितियाँ
ये सभी मिलकर पवनों की दिशा व गति निर्धारित करते हैं।
(vi) पवन के अपरदन कार्य से उत्पन्न स्थलाकतियों का वर्णन करें?
उत्तर- पवन के अपरदन कार्य से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।
शुष्क वायु द्वारा निर्मित अपरदित स्थलाकृति:-
1. वात गर्त/अपवाहन बेसिन
2. ज्यूगेन
3. यारडांग
4. गारा
5. छत्रक शिला
6. भूस्तंभ
7. मरुस्थलीय खिड़की
8. मरुस्थलीय पूल या मेहराव
9. ड्राई कान्टर
10. मरुस्थलीय बेसिन/अपवाह बेसिन
11. पेडीप्लेन एवं इंसेलवर्ग
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए
(i) पवन की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक बताएँ।
उत्तर- पवन की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं-
1. दाब प्रवणता बल (Pressure Gradient Force):-
वायुदाब के अंतर से पवन का निर्माण होता है। दो स्थानों के बीच दाब का अंतर जितना अधिक होगा, पवन की गति उतनी ही तेज होगी। दाब प्रवणता बल पवन को उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित करता है।
2. कोरिओलिस बल (Coriolis Force):-
पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवन की दिशा विक्षेपित होती है। उत्तरी गोलार्ध में पवन दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ता है। यह बल पवन की दिशा को प्रभावित करता है, लेकिन वेग को सीधे प्रभावित नहीं करता।
3. घर्षण बल (Frictional Force):-
पृथ्वी की सतह के नज़दीक पवन को भूमि सतह, पर्वत, वनस्पति और भवनों से घर्षण मिलता है, जिससे उसकी गति कम हो जाती है। ऊँचाई बढ़ने पर घर्षण कम हो जाता है और पवन का वेग बढ़ जाता है।
4. पृथ्वी का घूर्णन:-
पृथ्वी का घूमना पवनों की समग्र दिशा पर प्रभाव डालता है और वैश्विक पवन प्रणालियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
5. तापमान का वितरण:-
असमान तापमान वितरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में दाब भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे पवन की दिशा व गति प्रभावित होती है।
6. स्थानीय स्थलाकृति (Relief Features):-
पर्वतमाला, घाटियाँ, समुद्र–तट आदि पवन को मोड़ते हैं, बाधित करते हैं या उसकी गति बढ़ा देते हैं।
(ii) पथ्वी पर वायुमण्डलीय सामान्य परिसंचरण का वर्णन करते हए चित्र बनाएँ। 30० उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के सम्भव कारण बताएँ।
उत्तर- पृथ्वी पर वायुमण्डलीय सामान्य परिसंचरण (General Circulation of the Atmosphere) को तीन प्रमुख कोशिकाओं- हैडली, फेरल और ध्रुवीय कोशिकाओं-में विभाजित किया जाता है। यह परिसंचरण मुख्यतः पृथ्वी के असमान तापण, दाब-ढाल बल, कोरिओलिस प्रभाव तथा ऊर्ध्वनताप के अंतर के कारण विकसित होता है।
भूमध्यरेखा पर तीव्र तापण के कारण गर्म वायु ऊपर उठती है और निम्न दाब बनाती है। यह वायु ऊँचाई पर जाकर 30° उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है।
वहाँ पहुँचकर वायु ठंडी होकर नीचे उतरती है, जिससे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब (Subtropical High Pressure) का निर्माण होता है। इसके बाद सतह के निकट यह वायु भूमध्यरेखा और मध्य अक्षांशों की ओर लौटती है, जिससे व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें बनती हैं।
30° अक्षांशों पर उच्च दाब बनने के कारण
1. ठंडी होकर अवरोही गति- भूमध्यरेखा से उठी गर्म वायु ऊँचाई पर जाकर 30° अक्षांशों के पास ठंडी होकर नीचे आने लगती है।
2. कोरिओलिस प्रभाव- वायु के विस्तार को सीमित करता है, जिससे वायु एकत्र होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है।
3. ऊर्जा संतुलन- इस क्षेत्र में अवरोही वायु से आकाश साफ और शुष्क रहता है, जिससे उच्च दाब स्थिर रहता है।
(iii) उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर ही क्यों होती है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से किस भाग में मूसलाधार वर्षा होती है और उच्च वेग की पवनें चलती हैं, क्यों?
उत्तर- उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर इसलिए होती है क्योंकि इनके बनने के लिए अत्यधिक ऊष्मा एवं नमी की आवश्यकता होती है। समुद्र की सतह का तापमान लगभग 26.5°C या उससे अधिक होने पर जल का तीव्र वाष्पीकरण होता है, जिससे वातावरण में भारी मात्रा में जलवाष्प एकत्रित हो जाती है।
यह जलवाष्प ऊपर उठकर संघनित होती है और अंततः गुप्त ऊष्मा (latent heat) के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। यही ऊर्जा चक्रवात को शक्ति प्रदान करती है।
ठीक इसके विपरीत स्थलीय भागों पर इतनी नमी और ऊष्मा उपलब्ध नहीं हो पाती, इसलिए चक्रवातों की उत्पत्ति वहाँ नहीं होती।
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में मूसलाधार वर्षा और उच्च वेग की पवनें मुख्यतः आई-वॉल (Eye Wall) क्षेत्र में होती हैं। आई-वॉल चक्रवात का सबसे सक्रिय, ऊर्जावान और खतरनाक भाग होता है, जहाँ तीव्र ऊपर उठती वायु धाराएँ, अत्यधिक संघनन तथा भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होने से अत्यधिक वर्षा होती है।
इस क्षेत्र में दाब अत्यंत कम और दाब प्रवणता अत्यधिक तीव्र होने के कारण पवनें अत्यधिक वेग से बहने लगती हैं। इसके विपरीत, चक्रवात के केंद्र में स्थित आई (Eye) में मौसम अपेक्षाकृत शांत तथा वर्षा कम होती है।
इस प्रकार, समुद्री ऊष्मा, नमी और वायुदाब की भिन्नताएँ चक्रवात को जन्म देती हैं तथा आई-वॉल क्षेत्र को सबसे अधिक विनाशकारी बनाती हैं।