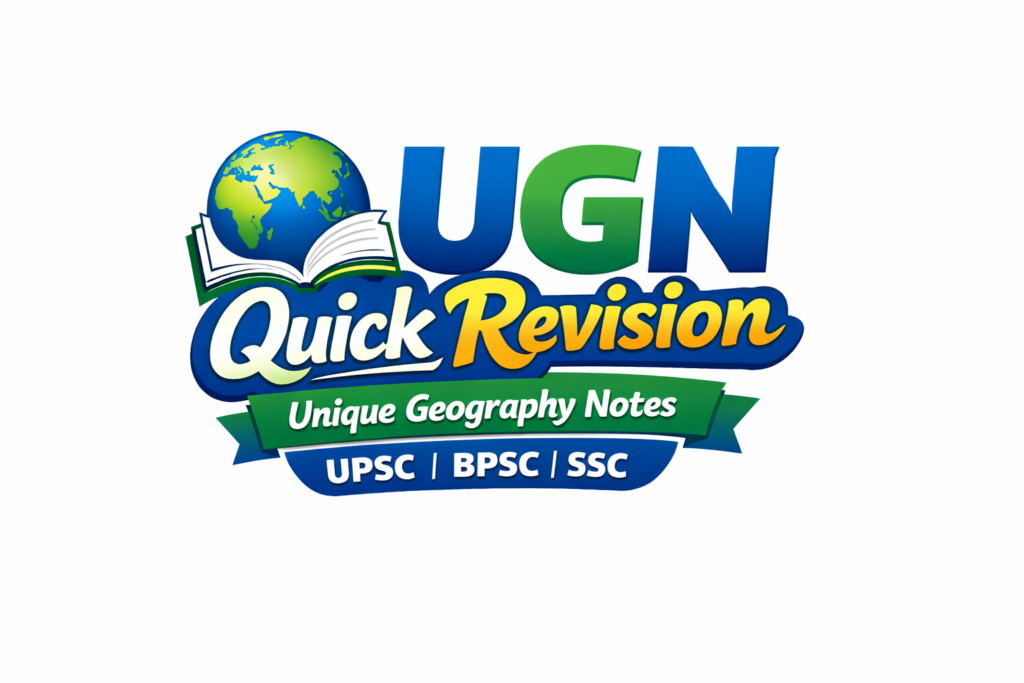26. Ecological Balance (पारिस्थितिक संतुलन)
Ecological Balance
(पारिस्थितिक संतुलन)
पारिस्थितिक संतुलन से तात्पर्य उस प्राकृतिक स्थिति से है, जहाँ सभी जैविक (Biotic) एवं अजैविक (Abiotic) घटक एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक के बीच ऊर्जा प्रवाह, पोषक तत्त्वों का चक्रण तथा पर्यावरणीय घटकों का परस्पर सहयोग शामिल होता है। जब यह संतुलन बना रहता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) स्थिर एवं सतत विकासशील बना रहता है।
पारिस्थितिक संतुलन के प्रमुख घटक
1. जैविक घटक (Biotic components)
(i) उत्पादक (Producers)- हरे पेड़-पौधे, शैवाल
(ii) उपभोक्ता (Consumers)- शाकाहारी (Herbivores), मांसाहारी (Carnivores) एवं सर्वाहारी (Omnivores) जीव
(iii) अपघटक (Decomposers)- कवक एवं जीवाणु
2. अजैविक घटक (Abiotic components)
⇒ वायु, जल, मृदा, सूर्य प्रकाश एवं खनिज
3. ऊर्जा प्रवाह (Energy Flow)
⇒ सूर्य से प्राप्त ऊर्जा खाद्य शृंखला के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर प्रवाहित होती है।
4. पोषक चक्र (Nutrient Cycle)
⇒ नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एवं जल चक्र पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखते हैं।
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के प्राकृतिक तंत्र
(i) खाद्य शृंखला (Food Chains) एवं खाद्य जाल (Food Webs):-
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में खाद्य शृंखला और खाद्य जाल का महत्वपूर्ण योगदान है। खाद्य शृंखला में एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जैसे-
घास
⇓
हिरण
⇓
बाघ
यह ऊर्जा के प्रवाह और पोषण चक्र को संतुलित करती है।

दूसरी ओर, खाद्य जाल कई खाद्य शृंखलाओं का जटिल रूप है, जिसमें विभिन्न जीव आपस में जुड़े रहते हैं। इससे यदि किसी एक जीव की संख्या घटती है तो अन्य विकल्प उपलब्ध रहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित नहीं होता। ये तंत्र जैव विविधता, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होते हैं।

(ii) जनसंख्या नियंत्रण (Population control):-
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जनसंख्या नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंत्र है। प्रकृति में हर जीव-जंतु और पौधों की संख्या सीमित रहती है, ताकि संसाधनों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। शिकारी-शिकार संबंध, भोजन की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन, रोग और परजीवी जैसे कारक स्वतः ही जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं।
उदाहरणस्वरूप, यदि किसी प्रजाति की संख्या अधिक हो जाए तो भोजन की कमी और शिकारी का दबाव उसे कम कर देता है। इसी प्रकार रोग और प्राकृतिक आपदाएँ भी जनसंख्या घटाने में सहायक होती हैं। ये प्राकृतिक नियंत्रण तंत्र जैव विविधता को बनाए रखकर पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करते हैं।
(iii) स्वयं नियमन (Self-regulation):-
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में प्राकृतिक तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण पहलू स्वयं नियमन (Self-regulation) है। इसमें जीवों की आबादी, संसाधनों का उपयोग और ऊर्जा प्रवाह स्वतः नियंत्रित होते हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में शिकारियों की संख्या बढ़ती है तो शिकार की जनसंख्या घट जाती है, जिससे शिकारियों की संख्या भी सीमित हो जाती है।
इसी प्रकार पौधों की वृद्धि जल, मिट्टी और सूर्य प्रकाश की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर बनाए रखती है और असंतुलन को रोकती है। इस प्रकार, स्वयं नियमन प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने की प्रमुख शक्ति है।
पारिस्थितिक असंतुलन के कारण
⇒ वनों की कटाई एवं मरुस्थलीकरण
⇒ प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि, मृदा)
⇒ अत्यधिक औद्योगीकरण एवं नगरीकरण
⇒ प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन
⇒ जलवायु परिवर्तन एवं ग्रीनहाउस प्रभाव
⇒ जैव विविधता का क्षरण
पारिस्थितिक असंतुलन के परिणाम
⇒ ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि और वैश्विक ऊष्मीकरण
⇒ ओजोन परत का क्षरण
⇒ प्रजातियों का विलुप्त होना
⇒ सूखा, बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि
⇒ कृषि उत्पादकता एवं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव
पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के उपाय
⇒ वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण
⇒ प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग
⇒ सतत कृषि एवं जल प्रबंधन
⇒ जैव विविधता संरक्षण
⇒ नवीकरणीय संसाधनों (सौर, पवन, जल विद्युत) का प्रयोग
⇒ पर्यावरणीय शिक्षा एवं जन-जागरूकता
⇒ “Reduce, Reuse, Recycle” की अवधारणा का पालन
निष्कर्ष:
इस प्रकार कहा जा सकता है कि पारिस्थितिक संतुलन मानव जीवन के अस्तित्व हेतु आवश्यक है। यदि मानव विकास की दौड़ में प्रकृति का संतुलन बिगाड़ता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल पर्यावरण पर, बल्कि समाज एवं अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है।
इसलिए आवश्यकता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर एवं सतत बना रहे।