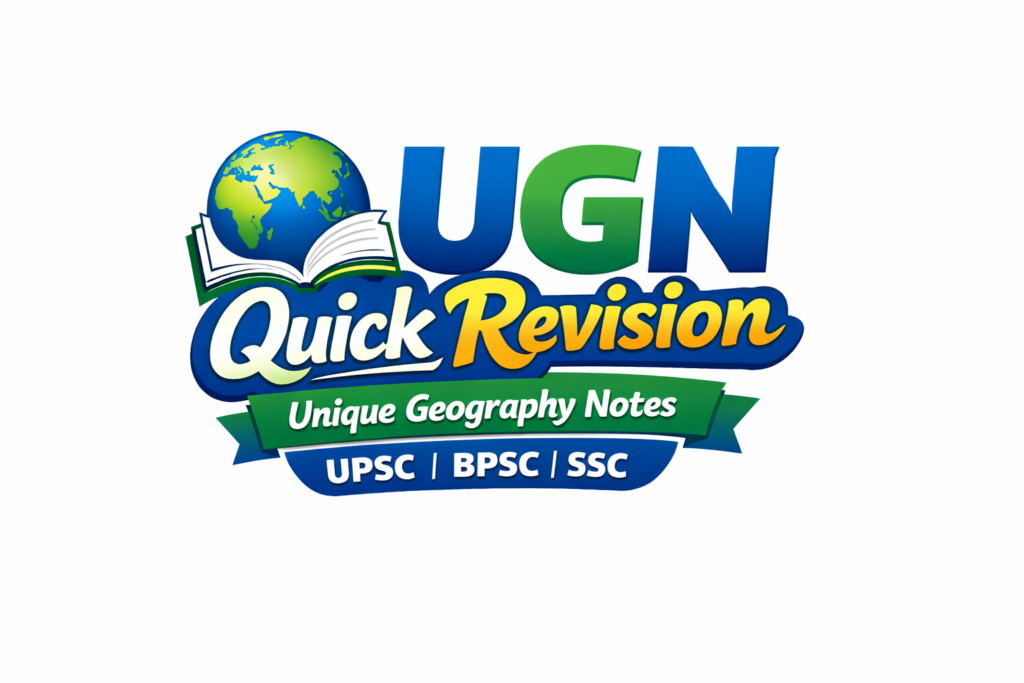24. Natural hazards and disasters (प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ)
Natural hazards and disasters
(प्राकृतिक खतरे और आपदाएँ)
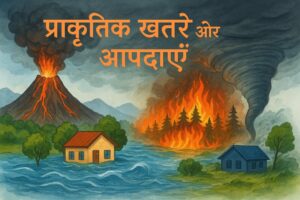
प्राकृतिक खतरों और आपदाओं में उन घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनसे जन-धन की अपार हानि होती है और जिनसे प्रलय एवं विनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उल्लेखनीय है कि मानव इन घटनाओं की उत्पत्ति को पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सका है।
प्राकृतिक खतरों और आपदाओं के अन्तर्गत ज्वालामुखी उद्गार, भूकम्प, भूस्खलन, टारनेडो, हरीकेन, चक्रवात, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और ब्लिजार्ड जैसी प्राकृतिक घटनाओं को सम्मिलित किया गया है। ध्यान रहे कि उपरोक्त उल्लेखित सभी घटनाएं उस समय पर्यावरणीय या प्राकृतिक आपदाओं का रूप लेती हैं जब इनसे मानव को भारी हानि होती है।
स्पष्ट है कि पर्यावरणीय आपदाओं की तीव्रता का निर्धारण उनके द्वारा होने वाली जन-धन की हानि की मात्रा के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, मानव रहित क्षेत्रों में भूकम्प एवं ज्वालामुखी उद्गार कभी भी आपदा के रूप में वर्णित नहीं किया जाता है, लेकिन जब कभी भूकम्प और ज्वालामुखी का उद्गार मानव आवासित क्षेत्रों में होता है तो ये प्राकृतिक घटनाएं आपदाओं के रूप में विवेचित की जाती हैं।
इसी प्रकार मानव जान-बूझकर भी इन प्राकृतिक घटनाओं से ग्रस्त क्षेत्रों को अपने आवास हेतु चुनता है। विश्व में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां मानव ने भूकम्पग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को अपने आवास-स्थल के रूप में पसन्द किया है। इस प्रकार के मानवीय निर्णय उसके अवबोध (Perception) से, कि वह किसी भी प्राकृतिक घटना का बोध कैसे करता है, प्रभावित होते हैं।
ज्ञातव्य है कि मानवीय अवबोध समय और संस्कृति (culture) के साथ बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, तिमोर सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में चक्रवातों से अपार जन-धन की हानि का भय सदैव बना रहता है।
1974 के भयंकर चक्रवात से हुई जन-धन की अपार हानि के उपरान्त डार्विन और उत्तरी आस्ट्रेलिया के निवासियों ने इस घटना का बोध कर अपने आवास हेतु अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित स्थलों को चुना है।
किसी भी प्राकृतिक घटना के बोध द्वारा ही इस बात का निर्धारण होता है कि या तो मानव उस आपदाग्रस्त क्षेत्र को छोड़ दे या फिर उस आपदा से होने वाली हानि को स्वीकार कर उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में ही रहे या फिर उस आपदा को कम करने के उपाय करे।
आपदा को कम करने के उपायों में व्यावहारिक भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो घटना की तीव्रता एवं आवृत्ति, इनकी उत्पत्ति के स्थल और उत्पत्ति के कारकों का ज्ञान करा मानव को इन घटनाओं को नियंत्रित करने के उपायों की ओर प्रवृत्त करती है।
मुख्य प्रकार:
1. बाढ़ (Floods) – अत्यधिक वर्षा या नदी के उफान से जलभराव।
2. ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption) – मैग्मा और गैसों का विस्फोट।
3. भूकंप (Earthquake) – धरती की सतह पर कंपन।
4. सुनामी (Tsunami) – समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल लहरें।
5. सूखा (Drought) – लंबे समय तक वर्षा न होना।
6. चक्रवात (Cyclone/Hurricane/Typhoon) – तेज हवाएँ और तूफान।
7. भूस्खलन (Landslide) – पर्वतीय ढलानों से चट्टानों या मिट्टी का खिसकना।
8. अत्यधिक तापमान (Extreme Temperature) – लू, शीतलहर, हीटवेव।
9. जंगल की आग (Forest Fire / Wildfire) – भारत में प्रमुख उदाहरण (जैसे उत्तराखंड या हिमाचल के जंगलों की आग)।
1. बाढ़ (FLOODING)
पर्यावरणीय अथवा प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़ एक सामान्य घटना है जो मानव को प्रभावित करती है विशेषकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में। जल की उपलब्धता, समतल भूमि की उपलब्धता, कृषि कार्यों में सुविधा तथा बाढ़ को एक आपदा के रूप में स्वीकार न करने के मानवीय बोध के कारण विश्व जनसंख्या का एक बड़ा भाग बाढ़ के मैदानों में रह रहा है।
उल्लेखनीय है कि मानव वायुमण्डलीय प्रक्रमों को नियंत्रित नहीं कर सकता है अर्थात् वह हरीकेन और चक्रवातों को तो आने से नहीं रोक सकता है, लेकिन जलवायवीय, भू-आकृतिक, जलीय और जैविक प्रक्रमों के सैद्धान्तिक ज्ञान का उपयोग कर बाढ़ जैसी आपदा को अवश्य नियंत्रित कर सकता है। एक अपवाह बेसिन में ढालों पर क्रियाशील प्रक्रमों और नदियों द्वारा उन प्रक्रमों के प्रति अनुक्रिया के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। यही घनिष्ठ सम्बन्ध नदी में बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु सैद्धान्तिक आधार प्रदान करता है।
बाढ़ जैसी आपदा को नियंत्रित करने के लिए वस्तुतः दो प्रकार के उपागमों को व्यवहार में लाया जाता है।
पहले उपागम (Approach) में बाढ़ को रोकने के सभी उपाय नदियों के उद्गम स्थल तथा ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए जाते हैं, जैसे:
(i) ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में ढालों को रूपान्तरित (Modified) करना,
(ii) नदी के उद्गम स्थल एवं ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वृहत् पैमाने पर वृक्षारोपण करना ताकि वर्षा जल का भूमि में अन्तः स्पन्दन (Infilteration) अधिक हो सके, फलतः वाही जल की मात्रा में कमी हो सके और वह विलम्ब से नदियों में पहुंचे।
वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन में कमी होने पर नदियों का अवसाद-भार तो कम होता ही है साथ ही नदियों की जलधारण क्षमता में कमी नहीं आने के कारण बाढ़ की आवृत्ति में भी कमी आती है और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का भी विस्तार नहीं हो पाता है।
दूसरे उपागम (Approach) के अन्तर्गत नदियों के मार्ग में ही बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाते हैं, जैसे :
(i) नदी के प्रवाह मार्ग में बाढ़ को नियन्त्रित करने हेतु भण्डारण जलाशयों अर्थात् बांधों का निर्माण करना।
(ii) नदियों के विसर्पाकार (Meandering) मार्ग को अभियांत्रिकी की सहायता से सीधा करना।
(iii) बाढ़ के समय अतिरिक्त जल के प्रवाह को निम्न भूमि (Low Land) या कृत्रिम रूप से निर्मित जलवाहिकाओं (Channels) में मोड़ देना।
(iv) जहां आवश्यक हो, वहां अभियांत्रिकी उपायों द्वारा नदियों के किनारों पर कृत्रिम तटबन्धों, डाइक (दीवार जैसी संरचना) और बाढ़-दीवाल (Flood wall) का निर्माण करना।
उपरोक्त उपायों के द्वारा नदियों में बाढ़ के समय जल के आयतन, उसकी ऊंचाई तथा परिमाण में कमी की जा सकती है। यद्यपि ये उपाय नदी की गति और उसके अपरदन तथा निक्षेपण कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वस्तु को बाढ़-प्रूफ (Flood-Proof) बनाने की बजाय समय पर बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी देकर मानव एवं पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना अधिक सुविधाजनक एवं सस्ता होता है।
2. ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption)
ज्ञातव्य है कि परिप्रशान्त मेखला तथा मध्य महाद्वीपीय मेखला के अन्तर्गत विश्व के 80 प्रतिशत ज्वालामुखी आते हैं और वस्तुतः विश्व के 80 प्रतिशत सक्रिय (Active) ज्वालामुखी विनाशकारी (Destructive) अभिसारी (Convergent) प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं।
यह सत्य है कि ज्वालामुखी के उद्गार को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके भावी उद्गार की भविष्यवाणी करके उसके द्वारा होने वाली जल-धन की हानि को अवश्य कम किया जा सकता है। इस हेतु निम्नांकित उपाय व्यवहार में लाए जा सकते हैं :
(i) सम्भावित ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में भूकम्प लेखी यंत्र द्वारा भकम्पीय घटनाओं के नियमित मापन से प्राप्त संकेतों के आधार पर भावी ज्वालामुखी उद्गार की भविष्यवाणी की जा सकती है।
(ii) मेग्मा तथा गैसों के भूगर्भ में नीचे से उपर की ओर उठने से धरातलीय सतह में उभार तथा झुकाव के रूप में विरूपण होने लगता है। विरूपण की यह मात्रा ज्वालामुखी उद्गार के पहले बढ़ती जाती है अतः सम्भावित क्षेत्रों में टिल्टमीटर की सहायता से धरातलीय सतह में झुकाव के नियमित मापन से भावी ज्वालामुखी उद्गार के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है।
(iii) सम्भावित ज्वालामुखी उद्गार के पहले तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस आधार पर क्रेटर झीलों, गर्म जल स्रोतों, गेसर एवं धुंआरों के जल के तापमान के नियमित मापन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भावी ज्वालामुखी उद्गार की भविष्यवाणी की जा सकती है।
(iv) स्थानीय गुरुत्व तथा चुम्बकीय क्षेत्र के मापन से प्राप्त परिणामों से सम्भावित ज्वालामुखी के उद्गार की भविष्यवाणी में सहायता मिलती है। स्मरणीय है कि उपरोक्त उपायों को व्यवहार में लाते हुए 1980 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में हुए सेण्ट हेलेन्स ज्वालामुखी के उद्गार की भविष्यवाणी पहले की जा चुकी थी। इस भविष्यवाणी के आधार पर व्यवहार में लाए गए सुरक्षात्मक उपायों के कारण ही इस ज्वालामुखी उद्गार से जन-धन की हानि अपेक्षाकृत कम हुई।
3. भूकम्प
भूकम्प प्राकृतिक भू-आकृतिक आपदा है। ज्ञातव्य है कि रचनात्मक प्लेट सीमाओं के सहारे मध्यम परिमाण वाले भूकम्प आते हैं जबकि उच्च परिमाण वाले भूकम्प विनाशी प्लेट सीमाओं के सहारे आते हैं, जहां पर दो अभिसारी प्लेट आपस में टकराते हैं तथा अपेक्षाकृत भारी प्लेट का हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण (Subduction) होता है।
इस दृष्टि से विश्व में परिप्रशान्त मेखला क्षेत्र, अल्पाइन-हिमालय पर्वत श्रृंखला के सहारे स्थित क्षेत्र तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी सीमान्त क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील हैं।
यद्यपि प्लेट के किनारों पर स्थित क्षेत्रों में भूकम्पीय घटनाएं सर्वाधिक होती हैं तथापि प्लेट के मध्यवर्ती भागों में भी कभी-कभी भूकम्प आते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की भांति ही भूकम्प को भी आने से रोका नहीं जा सकता है, किन्तु भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील भागों में मानव बसाव को हतोत्साहित करके भूकम्प द्वारा होने वाली जन-धन की हानि को अवश्य कम किया जा सकता है। साथ ही धरातलीय स्थिरता की दृष्टि से अस्थिर एवं कमजोर क्षेत्रों का निर्धारण करके उन क्षेत्रों में मानव बसाव को रोका जा सकता है।
4. सुनामी (Tsunami)
सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली अत्यधिक ऊँची और तीव्र गति से चलने वाली लहरों की शृंखला होती है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक खतरा है जो अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र के भीतर भूस्खलन या उल्का-पिंड के गिरने जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। जब यह खतरा मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी क्षति पहुँचाता है, तब यह एक प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेता है।
5. सूखा (Drought)
सूखा (Drought) एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो लंबे समय तक वर्षा के अभाव या अपर्याप्त वर्षा के कारण उत्पन्न होती है। यह प्राकृतिक खतरा कृषि, जल संसाधनों, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। सूखा केवल पानी की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक असंतुलन और पर्यावरणीय संकट का कारण भी बनता है।
6. चक्रवात (Cyclone/Hurricane/Typhoon)
जब समुद्र की सतह पर अत्यधिक गर्मी और नमी इकट्ठी हो जाती है, तो वायुमंडलीय दबाव कम होने लगता है और तेज़ हवाओं के साथ यह प्रणाली घूमती है। यही प्रक्रिया चक्रवात कहलाती है। चक्रवात एक प्राकृतिक आपदा है जो समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक नुकसान पहुँचाती है। इसके प्रबंधन हेतु पूर्वानुमान, चेतावनी प्रणाली, तटीय सुरक्षा दीवारें और राहत कार्य बेहद ज़रूरी हैं।
7. भूस्खलन (Landslide)
भूस्खलन (Landslide) प्राकृतिक खतरा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अचानक होने वाली प्राकृतिक भू-प्रक्रिया है, जिसमें भारी मात्रा में मिट्टी, चट्टानें और मलबा ढलान से नीचे की ओर खिसक जाते हैं। यह घटना अक्सर लोगों, पशुओं और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करती है। इसी कारण भूस्खलन को प्राकृतिक खतरा (Natural Hazard) की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह मानव जीवन, आजीविका, अवसंरचना और पर्यावरण सभी को प्रभावित करता है।
8. अत्यधिक तापमान (Extreme Temperature)
अत्यधिक तापमान (Extreme Temperature) को प्राकृतिक खतरा (Natural Hazard) इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली ऐसी चरम स्थिति है जो मानव जीवन, पशु-पक्षियों, कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
9. जंगल की आग (Forest Fire / Wildfire)
जंगल की आग (Forest Fire / Wildfire) को प्राकृतिक आपदा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होकर बड़े पैमाने पर पर्यावरण, जीव-जंतु, मानव जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुँचाती है।
निष्कर्ष:
स्पष्ट है कि प्राकृतिक भू-आकृतिक प्रकोपों के सम्भावित खतरों एवं प्रभावों के निर्धारण, भविष्यवाणी तथा आकलन एवं प्रबन्धन में भू-आकृति विज्ञान से पर्याप्त सहायता मिलती है।